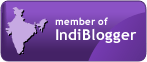मनुस्मृति धर्मकर्म या रिति-रिवाजों से संबंधित एक विवादास्पद ग्रन्थ है। इस ग्रंथ में बहुत-सी बातें हैं जिन पर आपत्ति नहीं की जा सकती है, बल्कि उन्हें स्वस्थ-सभ्य समाज के अनुरूप माना जायेगा। मनुस्मृति का “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते … “ कथन लोगों के मुख से अक्सर सुन्ने को मिलते हैं। निःसंदेह इस कथन में अनुकरणीय सलाह निहित है। किंतु इसी ग्रंथ में स्त्रियों के लिए कर्तव्याकर्तव्य की ऐसी अनेक बातें भी कही गई हैं जिसे महिला संगठन अमान्य कहेंगे। मैंने अपने वर्तमान ब्लॉग में मनुस्मृति पर आधारित तीन आलेख पहले कभी लिखे थे। देखें नारी संबंधी (2009-09-11), शुचिता संबंधी (2011-01-18), एवं शासकीय दंड संबंधी (2011-05-14) ब्लॉग प्रविष्टियां ।
https://vichaarsankalan.wordpress.com/2009/09/11/
https://vichaarsankalan.wordpress.com/2011/01/18/
https://vichaarsankalan.wordpress.com/2011/05/14/
मैं मौजूदा इस आलेख में हिन्दुओं में प्रचलित वर्ण-व्यवस्था के चतुर्थ वर्ण – “शूद्र” नाम से संबोधित – के बारे में मनुस्मृति के दो-चार श्लोकों का उद्धरण प्रस्तुत कर रहा हूं जिनमें नकारात्मक और “कदाचित्” आपत्तिजनक विचार व्यक्त किए गए हैं:
न शूद्रराज्ये निवसेन्नाधार्मिकजनावृते ।
न पाषण्डिगणाक्रान्ते नोपसृष्टेऽन्त्यजैर्नृभिः ॥
(मनुस्मृति, अध्याय 4, श्लोक 61)
(न शूद्र-राज्ये, न अधार्मिक-जन-आवृते, न पाषण्डि-गण-आक्रान्ते, न अन्त्यजैः नृभिः उपसृष्टे निवसेत्।)
अर्थ – (व्यक्ति को) शूद्र से शासित राज्य में, धर्मकर्म से विरत जनसमूह के मध्य, पाखंडी लोगों से व्याप्त स्थान में, और अन्त्यजों के निवासस्थल में नहीं वास नहीं करना चाहिए।
यहां व्यक्ति से तात्पर्य होना चाहिए उस व्यक्ति से जो वर्ण के अनुसार शूद्र से भिन्न हो, अर्थात वह जिसे आम तौर पर सवर्ण कहा जाता है (ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य)। धर्मकर्म से विरत उनको कहा जायेगा जो सवर्ण होते हुए धर्मानुकूल आचरण नहीं करते हैं। पाखंडी और धर्म-विमुख जनों में मुझे कोई अंतर नहीं दिखता। अंत्यज के अर्थ बहुत स्पष्ट नहीं हैं। मेरी समझ के अनुसार इस वर्ग में विधर्मी जनों को गिना जायेगा और उन्हें भी जो वर्णव्यवस्था को नकार कर अपनी स्वतंत्र व्यवस्था के अनुसार रहते हों। “चांडाल” को भी इसमें गिना जाता है, किंतु मैं चांडाल किसे कहा जाता है यह आज तक नहीं जान पाया! अस्तु।
आज के विशुद्ध भौतिकवादी युग में हर व्यक्ति का जीवनोद्येश्य एक ही है: किसी भी व्यवसाय से धनोपार्जन करना। कर्म के अनुसार देखा जाये तो किसी भी व्यक्ति का कोई वर्ण नहीं रह गया। वर्ण का अर्थ जातिसूचक शब्द रह गया है और धर्म स्वयं में दिखावा मात्र।
न शूद्राय मतिं दद्यान्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम्।
न चास्योपदिशेद्धर्मं न चास्य व्रतमादिशेत्॥
(मनुस्मृति, अध्याय 4, श्लोक 80)
(शूद्राय मतिम् न दद्यात्, न उच्छिष्टम्, न हविष्कृतम्, न च अस्य धर्मम् उपदिशेत्, न च अस्य व्रतम् आदिशेत्।)
अर्थ – किसी प्रयोजन की सिद्धि को ध्यान में रखते हुए दिया जाने वाला उपदेश शूद्र को न दिया जाये। उसे जूठा यानी बचा हुआ भोजन न दे और न यज्ञकर्म से बचा हविष्य प्रदान करे। उसे न तो धार्मिक उपदेश दिया जाये और न ही उससे व्रत रखने की बात की जाये।
जूठा का मतलब उस खाने से है जो किसी के लिए परोसा गया हो और छोड़ दिया गया हो। जूठे से तात्पर्य उस भोजन से नहीं लिया जाना चाहिए जो खाते-खाते थाली में बच जाये। यज्ञकर्म हेतु अग्निकुंड में जिस पदार्थ की आहुति दी जाती है उसे हविष्य कहा जाता है। यह घी या मक्खन हो सकता है, पर्वों पर बने पकवान हो सकते हैं, अथवा तिल, घी, चंदन-चूर्ण आदि का मिश्रण हो सकता है। व्रत से तात्पर्य है पापकर्मों से मुक्ति के निमित्त उपवास, दान, आदि के रूप में किए जाने वाला प्रायश्चित्त।
नाद्याच्छूद्रस्य पक्वान्नं विद्वानश्राद्धिनो द्विजः ।
आददीताममेवास्मादवृत्तावेकरात्रिकम्॥
(मनुस्मृति, अध्याय 4, श्लोक 223)
(विद्वान् द्विजः अश्राद्धिनः अस्य पक्व-अन्नम् न अद्यात्, अवृत्तौ अस्मात् एक-रात्रिकम् अमम् एव आददीत ।)
अर्थ – विद्वान् द्विज अश्राद्धिन् शूद्र द्वारा पकाया हुआ भोजन न खावे। परंतु तात्कालिक आर्थिक व्यवस्था न कर पाने की स्थिति में उससे एक रात्रि भर का कच्चा भोजन ग्रहण कर ले।
द्विज शब्द शूद्रेतर तीनों वर्णों के संस्कारित जन के लिए प्रयुक्त होता है। संस्कारित वह है जिसका उपनयन संस्कार हुआ हो। इस संस्कार के अंतर्गत व्यक्ति गुरु से शिक्षित होता है और ऐसा होना द्वितीय जन्म के तुल्य होता है। संस्कार के अभाव में व्यक्ति को पूर्व काल में शूद्र के तुल्य समझा जाता था। आज के युग में उपनयन की प्रथा बहुत कम प्रचलन में रह गयी है। ब्राह्मण जाति में भी यह परंपरा टूट रही है। इस दृष्टि से प्रायः सभी शूद्र हैं। अश्राद्धिन वह व्यक्ति है जो श्राद्ध आदि कर्म न करता हो; शूद्रों के लिए ये कार्य वर्जित कहे गये हैं। कच्चा भोजन वह है जिसे आग से न पकाया गया हो। आटा-दाल-चावल पकाये जाने से पहले कच्चे कहे जायेंगे।
न विप्रं स्वेषु तिष्ठत्सु मृतं शूद्रेण नाययेत्।
अस्वर्ग्या ह्याहुतिः सा स्याच्छूद्रसंस्पर्शदूषिता ॥
(मनुस्मृति, अध्याय 5, श्लोक 104)
(मृतम् विप्रंम् स्वेषु तिष्ठत्सु शूद्रेण न नाययेत्, सा शूद्र-संस्पर्श-दूषिता आहुतिः अस्वर्ग्या हि स्यात्।)
अर्थ – बंधु-बांधओं के उपलब्ध रहते हुए मृत ब्राह्मण का शरीर शूद्र के द्वारा बाहर न निकलवाए। शरीर के शूद्र के स्पर्श से दूषित होना ब्राह्मण के स्वर्गप्राप्ति में बाधक होती है।
यहां आहुति का क्या अर्थ है मैं समझ नहीं पाया। इन श्लोकों में शूद्र को खुलकर अस्पृश्य नहीं कहा गया है, किंतु जो कुछ कहा गया वह स्पष्ट करता है कि शूद्र कहे जाने वाले को शेष समाज हेय दृष्टि से देखता आ रहा है। सवर्णों का यह व्यवहार परंपरा के रूप में कब स्थापित हुआ होगा कहना मुश्किल है। कई “पंडित” जन ऋग्वेद के “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू …” (ऋग्वेद संहिता, मण्डल 10, सूक्त 90, ऋचा 12) एवं मनुस्मृति के “लोकानां तु विवृद्ध्यर्थं …” (मनुस्मृति, अध्याय 1, श्लोक 31) का उल्लेख करते हुए शूद्रों की हीनता को सिद्ध करते हैं। मैंने एक आलेख में ऋग्वेद के उक्त श्लोक की व्याख्या अपने प्रकार से की है (देखें ब्लॉग-प्रविष्टि 2013-9-26)
जो प्रचलित व्याख्या से पूर्णतः भिन्न है। मनुस्मृति के उपर्युक्त एवं अन्य कुछ कथन प्रचलित व्याख्या के पक्ष में जाते हैं। किंतु मेरा मत है कि वैदिक काल में स्थिति एकदम भिन्न रही होगी और पौराणिक काल से वर्ण-व्यवस्था में शनैःशनिः विकार आना शुरू हुआ होगा।
अस्तु, पाठक स्वविवेक से अपना मत नियत कर सकते हैं। -योगेन्द्र जोशी