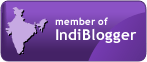मेरे पास “चाणक्यनीतिदर्पण” नामक पुस्तिका (ज्योतिष प्रकाशन, वाराणसी, २०००) है जिसमें अपने काल के सुविख्यात राजनीतिवेत्ता चाणक्य के छंद-निबद्ध नीतिवचन संकलित हैं, कुल ३४१ छंद १७ अध्यायों में वितरित। इन्हीं में से कुछ चुने हुए वचन यहां प्रस्तुत किए गये हैं।
[१]
यो ध्रुवाणि परित्यज्य ह्यध्रुवं परिषेवते ।
वाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव ही ॥अध्याय १-१३॥
[यः ध्रुवाणि परि-त्यज्य हि अ-ध्रुवम् परि-सेवते, ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति, अ-ध्रुम् नष्टम् एव ही ।] (ध्रुव = सुनिश्चित)
अर्थ – जिसकी सफलता पाना सुनिश्चित हो उस कार्य को छोड़कर जो व्यक्ति अन्य ऐसे कार्य में जुटता है जिसकी सफलता की संभावना क्षीण हो तो उसके लिए पहला कार्य तो निष्फल हो ही जाता है और दूसरे में भी विफलता निश्चित है।
कहते हैं “पूरी छोड़ आधी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे” । इसका उदाहरण आधुनिक जीवन के अंधी दौड़ में देखने को मिलती है। मैंने अनुभव किया है कि कई अभिभावक अपने बच्चे को जबरदस्ती डॉक्टर-इंजीनियर बनाने पर तुले रहते हैं जब कि उसकी रुचि किसी अन्य विषय – यथा लेखन, संगीत, या खेलकूद आदि – में रहती है। वे पहले में सफल हो नहीं पाते और समुचित प्रयास एवं अभ्यास के अभाव में दूसरा भी छूट चुकता है। अंत में हताशा हाथ लगती है।
[२]
परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम् ।
वर्जयेत्तादृशं मित्रं विषकुम्भपयोमुखम् ॥२-५॥
[परोक्षे कार्य-हन्तारम्, प्रत्यक्षे प्रिय-वादिनम्, वर्जयेत् तादृशम् मित्रम्, विष-कुम्भ-पयस् मुखम् ।] (प्रत्यक्ष = आंखों से सामने, परोक्ष = पीठ पीछे)
अर्थ – परोक्ष में जो काम बिगाड़ने की जुगत में लगा रहता है किंतु प्रत्यक्षतः यानी सामने मीठी-मीठी बातों से लुभाता है ऐसे मित्र से बचकर रहना चाहिए। वह विष से भरे उस घड़े के समान होता है जिसके मुख पर यानी उपरी हिस्से में दूध भरा है। अर्थात् ऐसा मित्र धोखा दे इसकी संभावन प्रबल होती है।
यह नीतिवचन बताता है व्यक्ति को बुद्धिमत्ता से यह पता लगाना चाहिए कि खुद को मित्र बताने वाला मनुष्य क्या वास्तविक सुहृद है। कई जन सामने मीठा-मीठा बोलने वाले होते हैं लेकिन पीठ पीछे स्वार्थवश अहित करने से नहीं चूकते। दरअसल वास्तविक हितैषी आमने-सामने कटु बोलने से नहीं परहेज नहीं करता यदि वह हितकर हो। वह अपने मित्र को सतही तौर पर खुश नहीं रखता।
[३]
दुर्जनस्य च सर्पस्य वरं सर्पो न दुर्जनः ।
सर्पो दंशति काले तु दुर्जनस्तु पदे पदे ॥३-४॥
[दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम् सर्पः न दुर्जनः, सर्पः दंशति काले तु, दुर्जनः तु पदे पदे ।]
अर्थ – दुर्जन मनुष्य एवं सांप में सांप ही अपेक्षया बेहतर है। सांप तो तब डंसता है जब समय वैसी परिस्थिति आ पड़े, किंतु दुर्जन तो पग-पग पर नुकसान पहुंचाता है।
दुर्जन वह है जिसके स्वभाव में सकारण-अकारण दूसरों को हानि पहुंचाना निहित होता है। जब भी मौका मिले वह दूसरे का अहित साधने में चूकता नहीं भले ही ऐसा करने में उसका कोई लाभ न हो। सांप ऐसी योजना नहीं बनाता; वह तो केवल अपने बचाव में डंसता है आवश्यक हो जाने पर।
[४]
लालयेत्पञ्चवर्षाणि दश वर्षाणि ताडयेत् ।
प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत् ॥३-१८॥
[लालयेत् पञ्च वर्षाणि, दश वर्षाणि ताडयेत् प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम् मित्रवत् आचरेत् ।] (यहां पुत्र = संतान)
अर्थ – मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी संतान को आरंभिक पांच वर्ष तक लाड़प्यार से पाले। उसके बाद दस वर्ष की आयु तक उसके साथ डांटडपट से पेश आये। किंतु संतान के सोलहवें वर्ष में पहुंचने पर उसके साथ मित्र की तरह व्यवहार करे।
यहां पर उल्लिखित पांच, दस, पंद्रह की संख्याओं को शब्दश: लेने की आवश्यकता नहीं। उक्त छंद मेरे मत में यह संदेश देता है कि शैशवावस्था एवं आरंभिक बाल्यावस्था में संतान को सही-गलत का ज्ञान नहीं होता। इस अवस्था में वह संसार से परिचित होता है और शनै:शनैः सीखता है कि क्या हानिकर है और क्या नहीं। इस काल में एक प्रकार से अज्ञानी होने के कारण बालक-बालिकाएं क्षमा एवं लाड़प्यार के अधिकारी होते हैं। परंतु इस उम्र के आगे उन्हें खतरों का एहसास होने लगता है और उन्हें अपने बड़ों से कोई काम करना ठीक होगा या नहीं की समझ मिलने लगती है। उम्र के इस अंतराल की शुरुआत में लाड़प्यार और डांटडपट-मारपीट दोनों को मौके की नजाकत के हिसाब से प्रयोग में लिया जाना चाहिए। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है ताड़ना कम और समझाना-बुझाना अधिक होते जाना चाहिए। अंत में युवावस्था में पहुंचते-पहुंचते बल-प्रयोग बंद करके माता-पिता को चाहिए कि संतान के साथ मित्र की भांति व्यवहार करे, अर्थात् बातचीत करते हुए और एक-दूसरे का दृष्टिकोण समझते हुए वे निष्कर्षों पर पहुंचें।
[५]
त्यजेद्धर्मं दयाहीनं विद्याहीनं गुरुं त्यजेत् ।
त्यजेत्क्रोधमुखीं भार्याम्निःस्नेहान्बान्धवांस्त्यजेत् ४-१६॥
[त्यजेत् धर्मम् दया-हीनम् विद्या-हीनम् गुरुम् त्यजेत् त्यजेत् क्रोध-मुखीम् भार्याम् निः-स्नेहान्-बान्धवान् त्यजेत् ।]
अर्थ – मनष्य को चाहिए कि उस धर्म को त्याग दे जिसमें दयाभाव न हो, उस गुरु को छोड़ दे जो विद्याहीन हो, मुख पर जिसके सदैव क्रोध झलकता हो ऐसी पत्नी को त्याग दे, और जिनके व्यवहार में स्नेह न हो उन बांधवों से मुक्त हो जावे।
धर्म के अर्थ बहुत व्यपक होते हैं। उसका एक पक्ष आध्यात्मिक ज्ञान होता है, लेकिन इस स्थल पर धर्म से तात्पर्य समाज एवं प्राणिजगत के प्रति आचरण से है ऐसा मेरा मानना है। (१) दूसरों के प्रति दयाभाव रखना इस आचरण में निहित होना चाहिए जो परोपकार के रूप में, मधुर वाणी में, निःस्वार्थ सेवा आदि में परिलक्षित हो। जिस सामाजिक तौर-तरीकों में यह आचरण न हो वह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। (२) गुरु वही होना चाहिए जो पढ़े-लिखे के आगे अनुकरणीय आचरण पेश करने की समझ रखे। उसका ज्ञान कोरी विद्या तक सीमित न हो। (३) असल पत्नी वही है जो मधुरभाषी एवं शान्त स्वभाव की हो। (४) अंत में नाते-रिश्तेदार परस्पर प्रेमभाव न रखें तो उनसे संबंध रखना व्यर्थ है। – योगेन्द्र जोशी