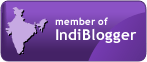प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में स्मृत्तियों का स्थान काफी महत्वपूर्ण रहा है। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा गया है। सबसे चर्तित रही है मनुस्मृति, जिसके कुछएक नीति वचन विवदास्पद भी रहे हैं। एक स्मृति और है याज्ञवल्क्यस्मृति जिसका महत्व भी काफी आंका जाता है। मेरे पास दोनों ही स्मृतिग्रंथ हैं। दोनों में अधिकांश बातें समान हैं। कुल स्मृतियां कितनी हैं यह मैं जान नहीं पाया हूं। मैंने नारदस्मृति, पराशरस्मृति एवं नारयणस्मृति का भी नाम भी सुना है, लेकिन उन्हें देखने-पढ़ने का अवसर अभी तक नहीं मिल सका है।
इन स्मृतियों में मनुष्य को परिवार और समाज के प्रति किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए इसका विस्तृत वर्णन मिलना है। समाज में अलग-अलग भूमिकाएं निभा रहे जनों के कर्तव्यों का लेखा-जोखा भी इन ग्रंथों में मिलता है। जैसे राजा के दायित्व क्या होने चाहिए और अधीनस्थों और प्रजा के प्रति उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए ये बातें स्पष्ट बताई गयीं हैं। स्थापित परंपराओं की चर्चा के साथ मनुष्य द्वारा उनके निर्वाह के उपदेश इन ग्रंथों में मिलते हैं। प्राचीन भारतीय वर्णश्रम व्यवस्था के अनुसार अलग-अलग वर्णों की सामाजिक भूमिकाओं और ब्रह्मचर्य से संन्यास आश्रम तक से संबंधित आचरण की विस्तृत व्याख्या इन ग्रंथों में निहित मिलती है।
उपर्युक्त दोनों स्मृतियों के अध्ययन से मुझे यही लगा कि ये स्मृतियां धर्म के आध्यात्मिक पक्ष को महत्व न देकर व्यावहारिक पक्ष की विस्तृत व्याख्या करती हैं। यह बात मेरे देखने में आई कि राजा के कर्तव्यों में विशेष महत्व न्यायकर्ता के तौर पर उसका अपराधियों के प्रति दंडात्मक रवैया अपनाना है। इस कार्य के लिए उसका दृडनिश्चयी एवं निष्पक्ष होना अनिवार्य है। याज्ञ्वल्क्यस्मृति में स्पष्ट उल्लिखित है जो व्यक्ति अनिश्चय की स्थिति में रहता हो वह राजा होने योग्य नहीं है। प्राचीन काल में तो राजा होता था, लेकिन आज के लोकतांत्रिक युग में चुने गये जनप्रतिनिधिगण सम्मिलित रूप से राजा की भूमिका निभाएं यह अपेक्षा की जाती है। वे कितना समर्पित होते हैं कर्तव्यो के प्रति यह संदेहास्पह अवश्य दिखाई देता है।
अपराधी को दंडित करना राजा के अनिवार्य कर्तव्यों में से एक है। इस बात का उल्लेख किंचित् विस्तार से याज्ञवल्क्यस्मृति के आचार नामक अध्याय के राजधर्मप्रकरण में किया गया है। मैं आगे प्रस्तुत अनुच्छेदों में के उक्त प्रकरण के चुने हुए ४ छंदों को अद्धृत कर रहा हूं जो राज्य की दंडात्मक प्रक्रिया से संबंधित हैं।
उक्त श्लोक वस्तुतः एक परिपूर्ण राज्य को परिभाषित करता है। राजा वह व्यक्ति होता है जो राजकीय व्यवस्था के शीर्ष पर होता है और व्यवस्था के दायित्व का निर्वाह करता है। मंत्रीगण एवं उनके सहायक अन्य सभी कर्मी राजा के नियंत्रण में राजकीय व्यवस्था चलाते हैं। प्रजा के अर्थ स्पष्ट हैं – राज्य की जनता। दुर्ग वह दुर्गम्य स्थान है जो शत्रुओं से राजा और मंत्रियों एवं अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करता है। राजकाज एवं जनहित के कार्यों के लिए संगृहीत राजस्व राजकोश कहलाता है। अपराधियों एवं भ्रष्ट जनों को दंडित करने की न्यायिक व्यवस्था दंड के अंतर्गत आती है। कोई भी राज्य तभी सुरक्षित होता है जब राज्य के भीतर एवं बाहर उसके हितैषी मित्र हों। आंतरिक तथा बाहरी शत्रु उस राज्य को कमजोर बनाते हैं, तब वह अपरिपूर्ण हो जाता है।
(१)
स्वाम्यमात्या जनो दुर्गं कोशो दण्डस्तथैव च ।
मित्राण्येताः प्रकृतयो राज्यं सप्ताङ्गमुच्यते ॥३५३॥
स्वामी, अमात्याः, जनः, दुर्गम्, कोशः, दण्डः, तथा एव च मित्राणि; एताः प्रकृतयः; राज्यम् सप्ताङ्गम् उच्यते।
स्वामी (राजा), मंत्रीवृंद, प्रजा, दुर्ग (किला), राजकोश, दंड, एवं राज्य के मित्रगण, ये सभी राज्य के सात अंग होते हैं। इसलिए राज्य को सप्तांग (सात अंगों वाला कहा गया है।
राज्य की उक्त सप्तांग परिभाषा प्राचीन काल की प्रचलित व्यवस्था का निरूपण है। आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजा एवं अमात्यों का स्थान प्रजा द्वारा चयनित जनप्रतिनिधियों की परिषद् ने ले लिया है। अन्य बातें कमोबेश वही हैं।
(२)
तदवाप्य नृपो दण्डं दुर्वृत्तेषु निपातयेत् ।
धर्मो हि दण्डरूपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा ॥३५४॥
तत् अवाप्य नृपः दण्डम् दुर्-वृत्तेषु निपातयेत्; धर्मः हि दण्ड-रूपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा।
ऐसा राज्य पा लेने पर राजा दुर्वृत्ति यानी दुराचरण में लिप्त जनों पर दंड गिराए (उन्हें दंडित करे)। वस्तुतः सृष्टिकर्ता ब्रह्म ने पहले (आरंभ में) धर्म का दंड के रूप में निर्माण किया था।
प्राचीन शासकीय व्यवस्थापकों और तत्संबंधित उपदेष्टाओं/चिंतकों ने दंड को शासन का अनिवार्य एवं प्रभावी अंग माना है। ध्यान दें कि राज्य के सात अंगों में “न्याय” (अंग्रेजी में “जस्टिस”) को नहीं शामिल किया है। उसके विपरीत अपराधी को दंड देने को महत्व दिया है। अगर गंभीरता से विचार करें तो आप समझ सकते हैं कि किसी भुक्तभोगी को “न्याय” देना लगभग असंभव होता है, क्योंकि जो “अनर्थ” किया जा चुका है उसे “न हुआ” अर्थात् निरस्त नहीं किया जा सकता है। जिसके प्राण लिए जा चुके हों उसे वापस नहीं ला सकते हैं। जिसे अकारण या अनुचित तरीके से कारागार में डाला गया हो, समय का उसका वह अंतराल वापस दिलाना संभव नहीं। जिसको मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ा हो उसकी कीमत आंकना संभव नहीं। इस प्रकार के अनेक दृष्टांत देखने को मिलेंगे जिससे “न्याय” की अवधारणा ही भ्रमात्मक सिद्ध होती है। “न्याय” शब्द यहां पर उसी अर्थ में लिया गया है जिस अर्थ में आम तौर पर प्रयोग में लिया जाता है।
संस्कृत भाषा में “न्याय” शब्द के मौलिक अर्थ इससे अधिक कुछ और हैं। “वामन शिवराम आप्टे के संस्कृत-हिन्दी शब्दकोश” में न्याय शब्द के अर्थ पर्याप्त विस्तार से बताये गये हैं। संक्षेप में इसका अर्थ वह तार्किक विधि या प्रणाली से है जो न्यायिक वाद के निस्तारण में सही निर्णय तक पहुंचने में अपनाई जाती है। न्यायिक व्यवस्था में “सच क्या है?” इसको जानने के लिए साक्षों पर आधारित तार्किक विधि ही तो अपनाई जाती है।
अपराधी को दंड दिया जा सकता है, समाज में स्थापित मूल्यों एवं मान्यताओं के अनुसार। इसीलिए प्राचीन धर्मग्रंथ-नीतिशास्त्र दंड को ही महत्व देते हैं। इसलिए उसी का उल्लेख नीति वचनों में मिलता है।
(३)
स नेतुं न्यायतोऽशक्यो लुब्धेनाकृतबुद्धिना ।
सत्यसन्धेन शुचिना सुसहायेन धीमता ॥३५५॥
सः नेतुम् न्यायतः अशक्यः लुब्धेन अकृत-बुद्धिना; सत्य-सन्धेन शुचिना सुसहायेन धीमता।
लोभी प्रकृति एवं अस्थिर बुद्धि वाले राजा के लिए दंड का प्रयोग न्यायपूर्वक कर पाना संभव नहीं है। सत्यनिष्ठ एवं निर्दोष आचरण वाले बुद्धिमान् राजा ही सद्व्यवहारी सहायकों के सहयोग से ऐसा कर सकता है।
जो राजा किसी निर्णय पर पहुंचते समय अपने निजी स्वार्थ पर ध्यान देता है, अथवा असमंजस की स्थिति में टिका रहता है, वह सही-सही दंड देने में समर्थ नहीं हो सक्ता है। राजा ऐसा हो जिसकी बुद्धि हर परिस्थिति में अविचलित रहे, जो दृढ़प्रतिज्ञ हो, स्थापित मियमों-परंपराओं पर टिका रहता हो। यह बात अगले श्लोक के प्रकाश में बेहतर समझ में आ सकती है। जैसा पहले कहा है, आज के लोकतांत्रिक युग में सत्ता पर आसीन जनप्रतिनिधि राजा का स्थान ग्रहण किए हुए हैं। यह अच्छी तरह देखने में आता है कि उनके निर्णय परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं और वे निष्पक्ष रह नहीं पाते।
(४)
अपि भ्राता सुतोऽर्घ्यो वा श्वसुरो मातुलोऽपि वा ।
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति धर्माद्विचलितः स्वकात् ॥३५८॥
अपि भ्राता, सुतः अर्घ्यः वा श्वसुरः मातुलः अपि वा, नादण्ड्यः नाम राज्ञः अस्ति धर्मात् विचलितः स्वकात्।
भाई, पुत्र, पूज्य जन, श्वसुर, एवं मामा, कोई भी अपने धर्म से विचलित होने पर राजा के लिए अदंडनीय नहीं होता है।
यह नीतिवचन स्पष्ट बताता है कि राजा के लिए निष्पक्ष बने रहना कितना कठिन हो सकता है, यदि उसका सामना नाते-रिश्तेदारों, मित्र-परिचितों आदि के अपराधों पर निर्णय देना होता है। उक्त छंद राजा को चेतावनी देता है कि शासकीय व्यवस्था में राजा के लिए कोई भी व्यक्ति अदंड्य, यानी जिसे दंडित होने से मुक्त रखा जा सके, नहीं होता। सामन्यतः जो उसका पूज्य होता है उसे भी अपराध करने पर दंडित करना राजा का कर्तव्य होता है। उसकी दृष्टि में जो भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों के निर्वाह करने में लापरवाही वरते वह अपराधी माना जायेगा। दंड हल्का-फुल्का अथवा गंभीर हो सकता है, लेकिन उसका अपराध राजा के दृष्टि में क्षम्य नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि राजा का ध्यान केवल अपराध और उसकी गंभीरता पर केन्द्रित होना चाहिए। वह अपराध पर ध्यान दे न कि इस पर कि अपराधी कौन है।
आधुनिक काल में सत्ता पर बैठे जनप्रतिनिधि स्वयं न्यायिक निर्णय नहीं लेते हैं, इसलिए उक्त बातें उन लोगों पर लागू होती हैं जिनके जिम्मे निर्णय लेना होता है। इस व्यवस्था में सत्तासीन जनों का कर्तव्य यह देखना होता है कि वे पूर्णतः निषक्ष रहकर निर्णय लें। ये बातें आदर्श की हैं और वास्तविक व्यावहारिक जीवन में कम ही देखने को मिलती हैं। – योगेन्द्र जोशी