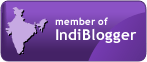वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद में तमाम देवी-देवताओं की प्रार्थनाएं हैं जिनमें इन्द्र एवं अग्नि प्रमुख हैं। दरअसल वैदिक मान्यता के अनुसार प्रकृति के सभी घटकों, जैसे जल, अग्नि, वायु, वर्षा, आदि के पीछे कोई न कोई चेतन दैवी शक्ति सक्रिय रहती है। सूर्य भी उनमें से एक है जो स्थूल रूप से प्रकाशित होने वाला आकाशीय पिंड का स्वामी है। सूर्य को कभी-कभी सविता के तौर पर भी पूजा जाता है जिसका तात्पर्य है कि वह प्राणियों की उत्पत्ति और उनके जीवन का आधार है। उसी सूर्य से स्वास्थ्य की कामना के तीन मंत्र (ऋचाएं) ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में मुझे पढ़ने को मिले हैं, जिनका उल्लेख मैं यहां पर कर रहा हूं। मेरी व्याख्या का आधार सायणाचार्य-कृत भाष्य (सायण-भाष्य) है जिसे मैंने अपने सीमित संस्कृत-ज्ञान के बल पर समझने का प्रयास किया है।
प्रार्थना का पहला मंत्र है –
उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिवम्।
हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय ॥११॥
(ऋग्वेद, मण्डल १, सूक्त ५०)
हे सूर्य प्राणियों के महान् मित्रवत् दीप्तिमान इस समय उदित होकर अंतरिक्ष (दिव) में ऊपर उठ रहे हो ऐसे तुम मेरे हृदयगत एवं दैहिक “हरिमाण” रोग का नाश करो।
यह ऋचा सूर्योदय के समय की जाने वाली प्रार्थना प्रतीत होती है। हृदयगत का तात्पर्य मानसिक रोग से है। इस मंत्र में “हरितवर्ण” वस्तुतः है क्या? सायण-भाष्य में इसकी दो प्रकार से व्याख्या की गई है। पहला, वह रोग जो शरीर के स्वाभाविक वर्ण को छीनकर उसे कांतिविहीन कर रहा हो (हर लिया है वर्ण यानी रंग जिसने)। रोगी का शरीर कांतिविहीन हो जाता है। उसके चेहरे की रौनक गायब हो जाती है। ऐसे रोग के नाश के लिए प्रार्थना की गई है। दूसरी व्याख्या है हरा वर्ण (रंग) यानी वह रोग जो शरीर का रंग हरा कर दे। आप्टे के शब्दकोश में हरित का अर्थ पीलापन भी दे रखा है। कदाचित् मंत्रद्रष्टा ऋषि का संकेत पीलिया की ओर होगा। प्रातःकालीन धूप रोगी के स्वास्थ्य के लिए कदाचित लाभकर हो।
अगला मंत्र है –
शुकेषु मे हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि ।
अथो हारिद्रवेषु मे अरिमाणं नि दध्मसि ॥१२॥
(यथोपर्युक्त)
मेरे शरीर के इस हरित-वर्ण के रोग को हम शुक (तोता) तथा शारिका (पक्षी विशेष का नाम) पक्षियों में स्थापित करते हैं। अथवा मेरे इस हरित-वर्ण रोग को हरे-पीले पेड़ों (कदंब?) पर हम स्थापित कर दें।
इस मंत्र का अर्थ मेरे लिए बहुत स्पष्ट नहीं है। भाष्य में रोपणाका का अर्थ शारिका दिया है, जिसे हिन्दी शब्दकोश में मैना कहा गया है। तोते का रंग हरा-पीला होता है किंतु मैना का रंग हल्का भूरा-सलेटी होता है। उसकी चोंच अवश्य ही सुर्ख पीली होती है। मुझे लगता है कि इस मंत्र के माध्यम से सूर्य की उपासना की जा रही है कि मेरे शरीर के रोगजनित हरित-वर्ण को मुझसे दूर करके उन्हीं पक्षियों, पेड़-पौधों तक सीमित रहने दो जिनके लिए यह रंग स्वाभाविक/प्राकृतिक है। अर्थात् मुझे रोगमुक्त कर दो।
तीसरी और अंतिम ऋचा ये है –
उदगादयमादित्यो विश्वेन सहसा सह ।
द्विषन्तं मह्यं रन्धयन्मो अहं द्विषते रधम् ॥१३॥
(यथोपर्युक्त)
अदिति-पुत्र आदित्य यहसूर्य पूरे बल से ऊपर अंतरिक्ष में चढ़ता है और मेरे प्रति उपद्रवकारी रोग का नाश करता है। मैं स्वयं उस द्वेषमय रोग के प्रति हिंसा नहीं करता।
मंत्र का अर्थ अपेक्षया सरल है। अर्थ कितना सारगर्भित है मैं कह नहीं सकता। कदाचित् मंत्रवक्ता रोग-निवारण का श्रेय प्रातःकालीन उदित हो रहे सूर्य को देता है जिसकी किरणें रोग से लड़ने में सहायक हों।
वैदिक प्रार्थनाएं कितनी कारगर होती हैं किसी प्रयोजन को सिद्ध करने में इसका कोई अनुभव मुझे नहीं है। किंतु इतना कहा जा सकता कि सूर्य की हल्की (प्रातःकालीन) धूप अवश्य ही स्वास्थ्य-वर्धक होती है। यही संदेश इन वैदिक ऋचाओं में दिखाई देता है। – योगेन्द्र जोशी
Tags: