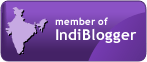परब्रह्म का पूर्ण ज्ञान किसी को है भी? – केनोपनिषद् में गुरु-शिष्य संवाद
वैदिक साहित्य में उपनिषदों को आध्यात्मिक ज्ञान के ग्रंथ कहा जाता है। यों तो बहुत से ग्रंथ हैं जिन्हें उपनिषद् कहकर संबोधित किया गया है जैसे सूर्योपनिषद्, मृतनादोपनिषद्, नारायणोपनिषद् आदि, किंतु केवल ११ उपनिषदों को ही प्रमुख उपनिषद् माना जाता है। ये उपनिषद् हैं –
(१) ईशावास्योपनिषद्
(२) ऐतरेयोपनिषद्
(३) कठोपनिषद्
(४) केनोपनिषद्
(५) छांदोग्योपनिषद्
(६) तैत्तिरिपनिषद्
(७) प्रश्नोपनिषद्
(८) माण्डूक्योपनिषद्
(९) मुण्डकोपनिषद्
(१०) वृहदारण्यकोपनिषद्
(११) श्वेताश्वतरोपनिषद्
इनमें वृहदारण्यक एवं छान्दोग्य उपनिषद् ग्रंथ अपेक्षया बड़े हैं। शेष सभी पर्याप्त छोटे हैं। सामान्यतः ये सभी भाष्य या टीका-टिप्पणी के साथ मुद्रित ग्रंथ के रूप में मिलते हैं। अन्यथा मंत्रों की संख्या तो बहुत कम रहती है, जैसे ईशोपनिषद् (ईशावास्योपनिषद्) में केवल १८ मंत्र हैं। कदाचित् यह उपनिषद् सर्वाधिक चर्चित है।
मैं इस आलेख में केनोपनिषद् के तीन मंत्रों का उल्लेख कर रहा हूं। इस उपनिषद् के दूसरे खंड में गुरु धर्मोपदेश देने के बाद शिष्य की परत्मात्म तत्व अर्थात् ब्रह्म की समझ के प्रति शंका व्यक्त करते हुए कहता है –
यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् ।
यदस्य त्वं यदस्य च देवेष्वथ नु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम् ॥१॥
(यदि मन्यसे सु-वेद इति दहरम् एव अपि नूनम् त्वम् वेत्थ ब्रह्मणः रूपम्, यद् अस्य त्वम्, यद् अस्य च देवेषु, अथ नु मीमांस्यम् एव ते मन्ये विदितम् ।)
यदि मानते हो कि तुम ब्रह्म के स्वरूप को भली भांति जान चुके हो तो तुम्हारा ज्ञान वस्तुतः अल्पमात्र, है। तुम में और देवताओं में परमात्मा के अंश की विद्यमानता का तुम्हारा ज्ञान अवश्य ही विचारणीय है (भले ही वह अपर्याप्त है)। [वेत्थ = जानते हो । मेरी जानकारी में यह आया कि कुछ ग्रंथों में ‘दहरम्’ के स्थान पर दभ्रम् मुद्रित मिलता है। दोनों के अर्थ एक ही हैं – अल्प।]
शिष्य गुरु को बताता है कि
नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च ।
यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च ॥२॥
(न अहम् मन्ये सु-वेद इति, नो न वेद इति, वेद च, यः नः तद् वेद तद् वेद नो न वेद इति वेद च ।) [वेद = जानता हूं; नो = नहीं; (उपसर्ग) सु = अच्छी तरह]
अंतिम सत्य के रूप में ब्रह्मतत्व को पूर्ण रूप से जान चुका हूं ऐसा मैं नहीं मानता। मैं नहीं ही जानता ऐसा भी नहीं; जानता भी हूं। हम शिष्यों में जो उसे (ब्रह्म को) जानता है वही मेरे उक्त कथन “नहीं जानता ऐसा भी नहीं है; जानता भी हूं” इसका आशय समझता है।
मुझे यह इस मंत्र का निहितार्थ पहेली जैसा लगता है। शिष्य का यह कहना कि मैं नहीं जानता ऐसी बात नहीं है क्योंकि मैं जानता भी हूं। कदाचित् शिष्य का यह कहना है कि वह परब्रह्म को पूर्णरूपेण जान चुका है ऐसा दावा वह नहीं कर सकता; उसे अभी अपनी समझ पूर्णता तक ले जाना है। अगले मंत्र में यह भाव कुछ-कुछ स्पष्ट हो जाते हैं।
यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः ।
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम् ॥२॥
(यथा पूर्वोक्त)
(यस्य अमतम् तस्य मतम्, मतम् यस्य न वेद सः अ-विज्ञातम् विजानताम् विज्ञातम् अ-विजानताम् ।)
परब्रह्म के ज्ञान का जिसका मत अव्यक्त है वही वस्तुतः जानता है। जो जान लेने का मत व्यक्त करता है वह वस्तुतः जानता नहीं है। जानने का अभिमान रखने वालों के लिए ब्रह्म जाना हुआ नहीं है और जो जानने का दावा नहीं करता वही उसे जानता है।
मुझे यह मंत्र भी एक पहेली-सा लगता है। कदाचित् कहने का प्रयास किया गया है कि ब्रह्मज्ञान भौतिक जगत् के सामान्य ज्ञान की भांति नहीं है। ब्रह्मज्ञान रहस्यमय है, अभौतिक-अलौकिक है, निर्वचनीय है, अभिव्यक्ति से परे है। असल ज्ञानी उसे जान लेने का अभिमान नहीं पालता। वह उसके बारे है कोई दावा करना उचित नहीं मानता है। यही संदेश कदाचित् इस मंत्र में दिया गया है। – योगेन्द्र जोशी