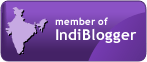बाल्मीकिकृत रामायण में ऋषि जाबालि एवं श्रीराम के बीच एक संवाद का जिक्र है जो मुझे रोचक लगा । प्रसंग है वनवास के लिए जा चुके श्रीराम को मनाने श्रीभरत का उनके पास नागरिकों के साथ जाना । श्रीभरत चाहते हैं कि वे अयोध्या लौटें और राजकाज सम्हालें । वे चाहते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में राज्य को लेकर जो अवांछित घटा उसे श्रीराम भूल जायें ।
राम-भरत के उस मिलाप के समय वहां ऋषि जाबालि भी मौजूद रहते हैं । श्रीराम इस बात पर जोर देते हैं कि वे अपने स्वर्गीय पिता को दिये गये वचन को तोड़कर उनकी आत्मा को कष्ट नहीं दे सकते । ऋषि जाबालि श्रीराम को समझाते हैं कि उन वचनों की अब कोई सार्थकता नहीं रह गयी और उन्हें व्यावहारिक उपयोगिता तथा जनसमुदाय की भावना को महत्त्व देना चाहिए । दोनों के बीच चल रहे तर्क-वितर्कों के दौरान एक समय ऋषि जाबालि कहते हैं कि मनुष्य दिवंगत आत्माओं के प्रति भ्रमित रहता है । वह भूल जाता है कि मृत्यु पर जीवधारी अपने समस्त बंधनों को तोड़ देता है । उसकी मृत्यु के साथ ही सबके संबंध समाप्त हो जाते हैं । न कोई किसी का पिता रह जाता है और न ही कोई किसी का पुत्र । संसार में छूट चुके व्यक्ति के कर्म दिवंगत आत्मा के लिए अर्थहीन हो जाते हैं । उन कर्मों से न उसे सुख हो सकता है और न ही दुःख । पर आम मानुष फिर भी भ्रम में जीता है । संवाद के दौरान वे कहते हैं, देखो क्या विडंबना है कि:
अष्टकापितृदेवत्यमित्ययं प्रसृतो जनः।
अन्नस्योपद्रवं पश्य मृतो हि किमशिष्यति ।।14।।
(बाल्मीकिविरचित रामायण, अयोध्याकाण्ड, सर्ग 108)
अष्टकादि श्राद्ध पितर-देवों के प्रति समर्पित हैं यह धारणा व्यक्ति के मन में व्याप्त रहती है, इस विचार के साथ कि यहां समर्पित भोग उन्हें उस लोक में मिलेंगे । यह तो सरासर अन्न की बरबादी है । भला देखो यहां किसी का भोगा अन्नादि उनको कैसे मिल सकता है वे पूछते हैं, और आगे तर्क देते हैं:
यदि भुक्तमिहान्येन देहमन्यस्य गच्छति ।
दद्यात् प्रवसतां श्राद्धं तत्पथ्यमशनं भवेत् ।।15।।
(पूर्वोक्त संदर्भ स्थल)
वास्तव में यदि यहां भक्षित अन्न अन्यत्र किसी दूसरे के देह को मिल सकता तो अवश्य ही परदेस में प्रवास में गये व्यक्ति की वहां भोजन की व्यवस्था आसान हो जाती – यहां उसका श्राद्ध कर दो और वहां उसकी भूख शांत हो जाये !
मुझे लगता है कि प्राचीन भारत में दर्शन एवं अध्यात्म के विषय में मनीषियों-चिंतकों का अपना स्वतंत्र मत होता था । उनके मतों में विविधता रहती थी, कदाचित् फिर भी उनके बीच गंभीर संघर्ष की स्थिति पैदा नहीं होती थी । जिसको जो मत भा जाये वह उसी को स्वीकार लेता था । यही कारण है कि इस देश में ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी एक साथ देखने को मिल जाते थे और हैं । वैमत्य तब तक घातक नहीं होता जब तक कि व्यक्ति असहमत व्यक्ति को कष्ट देना आरंभ न कर दे । संघर्ष की शुरुआत वस्तुतः तब होती है जब हम दूसरों पर अपने विचार थोपने लगते हैं, जैसा कि आज समाज में हो रहा है । मैं समझता हूं कि ऋषि जाबालि की आस्तिकता आम लोगों की आस्तिकता से भिन्न थी । – योगेन्द्र
(अष्टकादि श्राद्ध – कृष्णपक्ष की सप्तमी, अष्टमी, एवं नवमी की सम्मिलित संज्ञा अष्टक है । इन तीन दिनों के पितर-तर्पण आदि अष्टकादि श्राद्ध कहे जाते हैं ।)