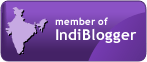संस्कृत ग्रंथ “पंचतंत्र” एवं “हितोपदेश” ऐसे दो ग्रंथ हैं जो छोटी-कथाओं के माध्यम से किशोरवय बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देने के उद्येश्य से लिखे गये हैं। इनमें से अधिकांश कथाएं इस प्रकार लिखी गई हैं कि एक के भीतर दूसरे का जिक्र आता है और दूसरी कथा उससे जुड़ जाती है। कथाओं की विशेषता यह है कि उनके पात्र प्रायः पशु-पक्षी हैं जो मनुष्यों की तरह बोलते एवं परस्पर संबंध निभाते हैं। इन पात्रों में वही गुण-अवगुण आरोपित रहते हैं जो मानव समाज में यत्रतत्र दिखाई देते हैं जैसे शत्रुता-मित्रता, सत्य-असत्य, उपकारिता-अपकारिता आदि के भाव। कहीं-कहीं पर मनुष्य पात्र भी शामिल दिखाई देते हैं। पंचतंत्र मौलिक ग्रंथ प्रतीत होता है किंतु हितोपदेश मुख्यतः अलग-अलग स्रोतों से लिए गये नीतिवचनों पर आधारित है जैसा कि स्वयं लेखक श्रीनारायणपंडित ग्रंथ के आरंभिक अनुच्छेदों से स्पष्ट होता है।
यहां पर मैं हितोपदेश के पांच छंदों/श्लोकों का उल्लेख कर रहा हूं। इनमें व्यक्त भावों का जिक्र हम सभी यदाकदा किसी न किसी मौके पर करते भी हैं।
(१)
नारिकेलसमाकारा दृश्यन्ते हि सुहृज्जनाः ।
अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोहराः ॥
(हितोपदेश, मित्रलाभ, ९४)
(सुहृत्-जनाः नारिकेल-सम-आकाराः हि दृश्यन्ते, अन्ये बदरिका-आकारा बहिः मनोहराः एव ।)
अर्थ – सहृदय यानी हितैषी जन नारियल की तरह (बाहर से) कुरूप होते हैं लेकिन अन्य लोग बेर-फल की तरह केवल बाहर से (चीकने-चुपड़े एवं )सुन्दर होते हैं।
नारियल जटाओं सदृश रेशों में लिपटा हुआ कड़े खोल वाला फल होता है जिसके भीतर मुलायम सुस्वादु गरी रहती है। इसके विपरीत बेर का बाहर का खोल (गूदा) देखने में सुन्दर एवं खाने में स्वादिष्ट होता है। किन्तु उसके भीतर कड़ी और निरुपयोगी गुठली होती है। ये उपमाएं यह दर्शाने के लिए चुनी गईं हैं कि असली मित्र (सुहृद) व्यवहार में अक्सर कठोर एवं रूखा होता है और दूसरे के लिए हितकर परंतु अप्रिय लगने वाली बात भी कह देता है। लेकिन उसका हृदय संवेदनशील, परोपकार भावना वाला और दूसरे के हित चाहने वाला होता है। अन्य लोग ऊपरी तौर पर मधुरभाषी (“पॉलिश्ड”) होते है किंतु वे दूसरों के हित की कामना रखते हों ऐसा कम ही होता है। वे जरूरत के समय कन्नी काट जाते हैं।
(२)
अधोऽधः पश्यतः कस्य महिमा नोपचीयते ।
उपर्युपरि पश्यन्तः सर्व एव दरिद्रति ॥
(हितोपदेश, सुहृद्भेद, २)
(अधः-अधः पश्यतः कस्य महिमा न उपचीयते, उपरि-उपरि पश्यन्तः सर्वः एव दरिद्रति ।)
अर्थ – अपने से नीचे देखने वाले किसकी महत्ता बढ़ नहीं जाती, और ऊपर-ऊपर देखने वाले सभी को अपनी दरिद्रता नजर आती है।
यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि समाज में व्यक्ति अपने को संपन्न-सुखी अनुभव करता है जब वह तुलनात्मक रूप से अपने से निम्नतर हालात वालों की ओर देखता है। उसे लगता है कि मैं कितनी अच्छी स्थिति में हूं। इसके विपरीत जब वह उनकी ओर देखता है जो उससे भी अधिक सम्पन्न-प्रतिष्ठित हों तो वह स्वयं को हीनतर अवस्था में पाता है। वस्तुतः मनुष्य की सुख-दुःख की अनुभूति दो प्रकार के कारणों से जुड़ी होती है। पहला कारण तो यह है कि उसकी मूलभूत आवश्यकताएं अपूरित रह रही हों, या वह अपनी समस्याओं का हल न खोज पा रहा हो, या भौतिक अथवा दैवी आपदाओं से घिरा हो, इत्यादि। दूसरा कारण समाज के अन्य सदस्यों से तुलना कर-कर के वह अपनी अवस्था से संतोष अथवा असंतोष प्राप्त करता है। ईर्ष्या मनुष्य के स्वभाव का एक अंग होता है जिसकी वजह से वह स्वयं को कभी सुखी तो कभी दुःखी अनुभव करता है। तुलना की इस प्रवृत्ति से पैदा हुए दुःख का कोई इलाज नहीं है।
(३)
स्वेदितो मर्दितश्चैव रज्जुभिः परिवेष्टितः ।
मुक्तो द्वादशभिर्वर्षैः श्वपुच्छः प्रकृतिं गतः ॥
(हितोपदेश, सुहृद्भेद, १३८)
(स्वेदितः, मर्दितः, एव रज्जुभिः परि-वेष्टितः च द्वादशभिः वर्षैः मुक्तः श्व-पुच्छः प्रकृतिम् गतः ।)
अर्थ – गर्म सिंकाई और मालिश की गयी, रस्सी से (सीधी रखने हेतु) लपेटकर रखी गयी, बारह वर्षों बाद खोली गयी तो भी कुत्ते की पूंछ अपने पूर्व स्वभाव में लौट आई।
सामान्य बोलचाल में भी हम ऐसी उक्ति का उल्लेख करते हैं “… कुत्ते की पूंछ टेड़ी की टेड़ी !” उपर्युक्त नीति वचन वस्तुतः इस तथ्य को व्यक्त करता है कि मानव स्वभाव बदलना आसान नहीं होता। सज्जन प्रकृति के लोगों को जब अपनी स्वभावगत कमियों का अहसास होता है, या अन्य जन उनके नकारात्मक पहलुओं की ओर संकेत करते हैं तो वह अपने में सुधार लाने का प्रयास करने लगते हैं। किंतु दुर्जन प्रकृति के लोग ढीठ होते हैं, सुधरने को तैयार नहीं होते हैं। आप प्रयास करते रहिए, वे अपनी आदत से मजबूर रहते हैं।
(४)
मत्तः प्रमत्तश्चोन्मत्तः श्रान्तः क्रुद्धो बुभुक्षितः ।
लुब्धो भीरुस्त्वरायुक्तः कामुकश्च न धर्मवित् ॥
(हितोपदेश, संधि, ५५)
(मत्तः, प्रमत्तः च उन्मत्तः, श्रान्तः, क्रुद्धः, बुभुक्षितः, लुब्धः, भीरुः, त्वरा-युक्तः, कामुकः च धर्म-वित् न ।)
अर्थ – मस्ती में डूबा हुआ (जैसे मदमस्त), लापरवाह (वस्तुस्थिति का होश न रहना), एवं उन्मादी (जुनूनी), थका हुआ, क्रोधित, भूखा, लोभी, कायर, जल्दबाज, और कामवासना से ग्रस्त व्यक्ति धर्मवेत्ता नहीं होता।
उक्त श्लोक में मनुष्य के उन दोषों का जिक्र किया गया है जो उसे धर्म से विमुख कर देते हैं, अर्थात् ऐसा व्यक्ति उचितानुचित का विवेक खो बैठता है। धर्म के प्रति समर्पित व्यक्ति का विवेकशील होना आवश्यक है ताकि वह शान्ति से उचित-अनुचित में भेद करे।
याद रहे कि धर्म का अर्थ कर्मकांड में लिप्त रहना नहीं। यदि आप प्राचीन ग्रंथों को गंभीरता से पढ़ें तो पाएंगे कि धर्म एक तरफ आत्मिक उत्थान से जुड़ा है तो दूसरी तरफ वह समाज, प्राणी-जगत और व्यापक स्तर पर प्रकृति के प्रति कर्तव्यों को व्यक्त करता है। देवी-देवताओं को पूजना, गंगास्नान करना, गेरुआ वस्त्र एवं तिलक आदि धारण करना इत्यादि धर्म के मूल तत्व नहीं होते।
(५)
दुर्जनदूषितमनसः सुजनेष्वपि नास्ति विश्वासः ।
बालः पायसदग्धो दध्यपि फूत्कृत्य भक्षयति ॥
(हितोपदेश, संधि, १०२)
(दुर्जन-दूषित-मनसः विश्वासः सुजनेषु अपि न अस्ति, पायस-दग्ध: बालः दधि अपि फूत्-कृत्य भक्षयति ।)
अर्थ – दुर्जनों द्वारा जिसका मन दूषित किया गया हो उसका विश्वास सुजनों में भी नहीं रह जाता है। (गर्म) दूध से जला बालक दही भी फूंक-फूंक कर पीता है।
एक सुपरिचित उक्ति है “दूध का जला छांछ फूंक-फूंककर पीता है।” उपर्युक्त छंद उसी भाव को व्यक्त करता है। उक्त छंद में दधि (दही) शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है मैं समझ नहीं पाया। दूषित मन वाले से तात्पर्य है जिसे दुर्जनों द्वारा धोखा दिया गया हो, जिसे भ्रमित करके छ्ला गया हो, जिसके साथ ज्यादती की गई हो, इत्यादि। फलतः वह व्यक्ति हर किसी के प्रति शंकालु हो जाता है। इसलिए धोखा खाया व्यक्ति संभल-संभल कर चलता है। उसकी स्थिति दूध के जले निरीह बालक की सी होती है जो ठडे छांछ को भी गर्म दूध की तरह समझकर उसे फूंक-फूंककर पीता है।
बहुत से लोग परेशानी में पड़े व्यक्ति की सहायता करते हैं। लोगों की इस प्रवृत्ति का चालाक-मक्कार जन नाजायज फायदा उठाते हैं। सीधे-सादे आदमी को जब पता चलता है कि उसे धोखा दिया गया है तो वह घटना से सबक लेते हुए भविष्य में सावधान हो जाता है। जिनको मदद की वास्तव में जरूरत होती है उन पर भी शंका करते हुए मदद करने भी बचता है। किसी के माथे पर सज्जनता या दुर्जनता का ठप्पा तो लगा नहीं रहता! दुर्जनों के कारण सज्ज्नों को भी हानि उठानी पड़ती है। – योगेन्द्र जोशी