वैदिक ग्रंथ ‘मुंडक उपनिषद्’ में परब्रह्म के स्वरूप और उसे प्राप्त करने के मार्ग का वर्णन किया गया है । माना जाता है कि यह ग्रंथ प्रमुखतया उन आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है जो मोक्ष की समझ और उसकी प्राप्ति का मार्ग जानना चाहते हैं । वैदिक दार्शनिेकों के मतानुसार जीवधारियों का भौतिक पदार्थों से बना स्थूल शरीर तो नश्वर है, किंतु उसमें ‘निवास’ करने वाली अमूर्त आत्मा अमर है । स्थूल स्तर पर नाशवान शरीर की जिस मृत्यु का अनुभव हम करते हैं वह वस्तुतः आत्मा का शरीर छोड़ना भर है । वास्तव में आत्मा वारंवार शरीर धारण करती है और कालांतर में उसे छोड़ती है । वह जन्म-मरण के चक्र से बंधी रहती है । प्राचीन वैदिक चिंतक मानने थे कि परमात्मा या परब्रह्म समस्त सृष्टि का मूल है और आत्मा वस्तुतः उसका एक अंश है । परब्रह्म और आत्मा के बीच का संबंध कुछ-कुछ वैसा ही है जैसा विशाल समुद्र और उससे विलग हुई जल की एक बूंद का । अपनी देह से संपादित कर्मफलों के बंधन से आत्मा जन्ममरण के चक्र में तब तक भटकती रहती है जब तक कि उसे अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात् परब्रह्म का अंश होने का ज्ञान नहीं हो जाता है । ज्ञानप्राप्ति के पश्चात वह उसी में लीन हो जाती है । उस अवस्था को माक्ष की संज्ञा दी गई है । सामान्य शब्दों में अभिव्यक्त इस दार्शनिक विचार के गहरे अर्थ समझना किस-किस के लिए संभव है यह मैं नहीं कह सकता ।
आत्मा के सही स्वरूप का ज्ञान किसे और कैसे मिलता है इस बात का उल्लेख मुंडक उपनिषद के अधःप्रस्तुत तीन मंत्रों में मिलता है:
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् ।।3।।
(मुण्डकोपनिषद्, मुंडक 3, खंड 2)
(न अयम् आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन, यम् एव एषः वृणुते तेन लभ्यः, तस्य एषः आत्मा विवृणुते तनुम् स्वाम् ।)
अर्थ – यह आत्मा प्रवचनों से नहीं मिलती है और न ही बौद्धिक क्षमता से अथवा शास्त्रों के श्रवण-अध्ययन से । जो इसकी ही इच्छा करता है उसेयह प्राप्त होता है, उसी के समक्ष यह आत्मा अपना स्वरूप उद्घाटित करती है ।
यहां आत्मा को पाने का अर्थ है आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना । धार्मिक गुरुओं के प्रवचन सुनने से, शास्त्रों के विद्वत्तापूर्ण अध्ययन से, अथवा ढेर सारा शास्त्रीय वचनों को सुनने से यह ज्ञान नहीं मिल सकता है । इस ज्ञान का अधिकारी वह है जो मात्र उसे पाने की आकांक्षा रखता है । तात्पर्य यह है कि जिसने भौतिक इच्छाओं से मुक्ति पा ली हो और जिसके मन में केवल उस परमात्मा के स्वरूप को जानने की लालसा शेष रह गयी हो वही उस ज्ञान का हकदार है । जो एहिक सुख-दुःखों, नाते-रिश्तों, क्रियाकलापों, में उलझा हो उसे वह ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है । जिस व्यक्ति का भौतिक संसार से मोह समाप्त हो चला हो वस्तुतः वही कर्मफलों से मुक्त हो जाता है और उसका ही परब्रह्म से साक्षात्कार होता है ।
नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिंगात् ।
एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वान्स्तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम ।।4।।
(यथा पूर्वोक्त)
(न अयम् आत्मा बल-हीनेन लभ्यः न च प्रमादात् तपसः वा अपि अलिंगात् एतैः उपायैः यतते यः तु विद्वान् तस्य एषः आत्मा विशते ब्रह्म-धाम ।)
अर्थ – यह आत्मा बलहीन को प्राप्त नहीं होती है, न ही धनसंपदा, परिवार के विषयों में लिप्त रहने वाले को, और न तपस्यारत किंतु संन्यासरहित व्यक्ति को । जो विद्वान एतद्विषयक उपायों को प्रयास में लेता है उसी की आत्मा परब्रह्मधाम में प्रवेश करती है ।
यहां पर बलहीन का अर्थ सामान्य दैहिक अथवा बौद्धिक बल से नहीं है । जिसके पास आत्मसंयम का सामर्थ्य है वही बलवान है क्योंकि वह विपरीत परिस्थिति में भी अविचलित रह सकता है । किंतु ऐसा व्यक्ति भी मोक्ष्य के योग्य नहीं होता । संन्यास का अर्थ है सांसारिक बंधनों से स्वयं को मुक्त करना । जिस व्यक्ति को कोई लालसा नहीं, जो संभी बंधन तोड़ चुका हो, जिसका न कोई अपना रह गया हो और न पराया वह वीतराग संन्यासी कहलाता है । ऐसा संन्यासी बनना ही परब्रह्म के ज्ञान का उपाय है ।
संप्राप्यैनमृषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागः प्रशान्ताः ।
ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति ।।5।।
(यथा पूर्वोक्त)
(संप्राप्य एनम् ऋषयः ज्ञान-तृप्ताः कृत-आत्मानः वीत-रागः प्रशान्ताः ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीराः युक्त-आत्मानः सर्वम् एव आविशन्ति ।)
अर्थ – आत्मा के यथार्थ को पा लेने पर ऋषिगण ज्ञानतृप्त, कृतकृत्य, विरक्त, और परम शान्त हो जाते हैं । वे धीर पुरुष उस सर्वव्यापी परब्रह्म को सर्वत्र प्राप्त करते हुए और उससे युक्तचित्त होकर उसी संपूर्ण ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं, यानी उससे एकाकार हो जाते हैं ।
इस मंत्र की व्याख्या में कहा गया है कि आत्मा के मूलस्वरूप का ज्ञान पा चुकने वाले ऋषि के लिए उसका शरीर एक अस्थाई सांसारिक बंधन रह जाता है । उसके लिए देहत्याग पर परब्रह्म में लीन होना वैसा ही होता है जैसा किसी घड़े के टूटकर बिखरने पर उसके भीतर के आंशिक आकाश और बाह्य असीमित आकाश के बीच का भेद समाप्त हो जाता है । युक्तचित्त की स्थिति में केवल ब्रह्म का ही भाव उसके मन में रह जाता है और सांसारिक समस्त वस्तुओं में उसी ब्रह्म के दर्शन होने लगते है । उसके लिए कुछ भी सांसारिक बांछनीय नहीं रह जाता है । प्राचीन काल में वैदिक चिंतकों को कदाचित घड़े का दृष्टांत ही उपयुक्त लगा होगा । आज विकल्पतः हवा भरे गुब्बारे का दृष्टांत सोचा जा सकता है जिसके, भीतर का आकाश बाह्य आकाश से पूरी तरह विभक्त रहता है । – योगेन्द्र जोशी


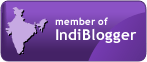

सितम्बर 11, 2014 @ 09:40:03
बढ़िया
फरवरी 10, 2015 @ 04:46:56
स्मृ्ति तो निर्विकार आत्मा ही है, लेकिन जब उसमे जीवत्व(मै शरीर हूँ या ये शरीर मेरा है, ये भाव) प्रक्ट होने लगता है तो वही जीव की स्मृति कही जाती है ।
जय श्री कृष्ण
जून 21, 2019 @ 16:50:29
जन-ज्ञान वर्धन के लिए आपका धन्यवाद. संयुक्त शब्दों का संधि-विच्छेद कर और उनका शब्दश: अर्थ बता कर आपने विषय को सरल बना दिया है. संयुक्त शब्दों का बड़ा आकार देख कर सामान्य समाज हतोत्साहित हो जाता है कि वेद-वांग्मय को समझना हमारे बस की बात नहीं. पुन: आपका आभार.
जनवरी 22, 2020 @ 11:01:20
“Needs easy words …” से आपका क्या मतलब है मैं समझ नहीं पाया।
मैं जब हिन्दी में लिखता हूं तो उसमें अंग्रेजी के शब्दों की भरमार पसंद नहीं करता ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजी में लिखते समय हिंदी या अन्य भाषाओं के शब्दों को उसमें “घुसेड़ता” नहीं।
आजकल लोग हिन्दी तो ठीक से जानते नहीं और अपनी बात बिना अंग्रेजी शब्दों के कह नहीं सकते। लेकिन अंग्रेजी बोलने और लिखने में बहुत सचेत रहते हैं ताकि उसमें कोई गलती न हो। लेकिन हिन्दी को “घर की मुर्गी दाल बराबर” की तर्ज पर शुद्ध हिन्दी की क्या जरूरत सोचते हैं। लेकिन मैं अपनी नीति बदल नहीं सकता !