“अहिंसा परमो धर्मः” प्राचीन संस्कृत साहित्य में उपलब्ध नीति-वचनों में से एक है जिसका उल्लेख अहिंसा के पक्षधर लोग अक्सर करते हैं। इस विषय में महाकाव्य महाभारत के तीन श्लोकों का उल्लेख मैंने अपने पिछली चिट्ठा-प्रविष्टि (ब्लॉग-पोस्ट) में किया था। मौजूदा आलेख में उसी महाभारत ग्रंथ के अन्य तीन श्लोकों को उद्धृत कर रहा हूं जो मुझे ग्रंथ में पढ़ने को मिले। इनकी चर्चा के बाद अहिंसा कितना अव्यावहारिक विचार है इस पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। पहले श्लोक:
अहिंसा परमो धर्मस्तथाहिंसा परो दमः ।
अहिंसा परमं दानमहिंसा परमं तपः ॥28॥
(महाभारत, अनुशासन पर्व, अध्याय 116, दानधर्मपर्व)
(अहिंसा परमः धर्मः तथा अहिंसा परः दमः अहिंसा परमम दानम् अहिंसा परमम् तपः ।)
शब्दार्थ – अहिंसा परम धर्म है, वही परम आत्मसंयम है, वही परम दान है, और वही परम तप है।
अहिंसा परमो यज्ञस्तथाहिंसा परं फलम् ।
अहिंसा परमं मित्रमहिंसा परमं सुखम् ॥29॥
(यथा पूर्वोक्त)
(अहिंसा परमः यज्ञः तथा अहिंसा परम् फलम् अहिंसा परमम् मित्रम् अहिंसा परमम् सुखम् ।)
शब्दार्थ – अहिंसा परम यज्ञ है, अहिंसा ही परम फल है, वह परम मित्र है, और वही परम सुख है।
सर्वयज्ञेषु वा दानं सर्वतीर्थेषु वाऽऽप्लुतम् ।
सर्वदानफलं वापि नैतत्तुल्यमहिंसया ॥30॥
(यथा पूर्वोक्त)
(सर्व-यज्ञेषु वा दानम् सर्व-तीर्थेषु वा आप्लुतम् सर्व-दान-फलम् वा अपि न एतत् अहिंसया तुल्यम् ।)
शब्दार्थ – सभी यज्ञों में भरपूर दान-दक्षिणा देना, या सभी तीर्थों में पुण्यार्थ स्नान करना, या सर्वस्व दान का फल बटोरना, यह सब अहिंसा के तुल्य (समान फलदाई) नहीं हैं।
ऊपरी तौर पर देखें तो इन श्लोकों में कोई प्रभावी बात नहीं दृष्टिगत होती है। अहिंसा परम धर्म, परम आत्मसंयम, परम दान एवं परम तप है (उपर्युक्त प्रथम श्लोक) कहने का तात्पर्य यही लिया जा सकता है कि धर्म के अंतर्गत आने वाले सभी सत्कर्मों में अहिंसा प्रथम यानी सर्वोपरि है। अहिंसा का व्रत सरल नहीं हो सकता। अहिंसा में संलग्न व्यक्ति धर्म-कर्म की अन्य बातों पर भी टिका ही रहेगा। शायद यही इस श्लोक का संदेश है।
आम तौर पर हवनकुंड की प्रज्वलित अग्नि में हविष्य (हवन-सामग्री) की आहुति देकर देवताओं की प्रार्थना को यज्ञ कहा जाता है। लेकिन यज्ञ के इससे अधिक व्यापक अर्थ भी हैं। वस्तुतः पूजा-अर्चना से परे अन्य पुण्यकर्म करना भी यज्ञ कहलाता है। मनुस्मृति में पांच महायज्ञों का जिक्र पढ़ने को मिलता है: ये हैं:
ब्रह्मयज्ञ – अध्यापन-कार्य अर्थात् लोगों का ज्ञानवर्धन करना।
पितृयज्ञ – पितृ-तर्पण अर्थात् पितरों का स्मरण एवं श्रद्धा अभिव्यक्ति।
होमकार्य – दैवयज्ञ यानी देवताओं की पूजा अर्चना, यज्ञ-यागादि। (दैवयज्ञ)
भूतयज्ञ – बलिप्रदान अर्थात् अन्य प्राणियों को अपने भोजन का एक अंश, जिसे बलि कहते हैं, अर्पित करना।
नृयज्ञ – विविध प्रकार से अतिथियों का सत्कार, जिसमें भोजन प्रमुख है।
इन महायज्ञों के विषय पर मैंने इसी ब्लॉग पर दो आलेख (31 मार्च, 2015 एवं 16 मार्च, 2015) विगत काल में पोस्ट की थीं।
इस स्थल पर आम आदमी के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या अहिंसा वाकई में धर्म का श्रेष्ठतम कर्म है। उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि धर्म का क्या अर्थ है और उसके पालन का क्या उद्देश्य है। प्राचीन भारतीय चिंतकों का मत रहा है कि मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना है। अर्थात् जीवन-मरण के निरंतर चलने वाले चक्र से स्वयं को मुक्त करना। इसके लिए स्वयं का आध्यात्मिक उत्थान और इस संसार के मोह से अपने को बचाना है। इसके लिए आत्मिक परिष्करण और शेष संसार के प्रति सत्कर्म करना ही मार्ग है यह उनका मत रहा है। लोकायत परंपरा (चार्वाक सिद्धांत) को छोड़कर अन्य सभी धार्मिक मत एक ही प्रकार से सोचते हैं, अंतर है तो आध्यात्मिक दर्शन में और सत्कर्मों की परिभाषा तथा उनकी परस्पर सापेक्ष वरीयता में। लोकायत में तो इस भौतिक शरीर से परे कुछ नहीं है और तदनुसार कर्मों का महत्व व्यक्ति एवं समाज के परस्पर रिश्तों के संदर्भ में होता है। इसके विपरीत जैन मत में जीवधारी सत्कर्मों के फलस्वरूप उत्तरोत्तर श्रेष्ठतर अवस्था प्राप्त करते हुए अंत में मुक्तजीव हो जाता है; बौद्ध मत में जीवधारी का कर्मशरीर शून्य में विलीन हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता; और वैदिक दर्शन में जीवधारी की आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, इत्यादि।
आध्यात्मिक उत्थान के लिए मनुष्य के लिए सत्कर्मों का संपादन आवश्यक है और उपर्युक्त श्लोकों में वही संदेश मुझे दिखता है।
मेरा मानना है कि दुनियाबी जिंदगी में अहिंसा स्वीकार्य नहीं हो सकती है। हिंसा मनुष्य के स्वभाव का अपरिहार्य अंग है और आत्मसंयम द्वारा विरले जन ही उसे नियंत्रित कर पाते हैं। व्यवहार में अहिंसा पर टिके रहना आम जन के लिए असंभव है। यह निर्विवाद तथ्य है कि सामाजिक व्यवस्था सुचारु बनाए रखना हिंसा को नकारने पर असंभव है। हिंसा का प्रयोग यथासंभव कम एवं विवेकपूर्ण तरीके से करना सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। यह हिंसा ही है जिससे मनुष्य डरता है और सन्मार्ग पर टिकने के लिए विवश होता है।
उपर्युक्त श्लोक जिस महाभारत ग्रंथ में मिलते हैं उसी में सर्वत्र हिंसा के तमाम दृष्टांतों का उल्लेख है। इतना ही नहीं, इसी ग्रंथ में हिंसा की अपरिहार्यता की बातें भी कही गयी हैं। इसी प्रकार वाल्मिकीय रामायण भी हिंसात्मक घटनाओं का लेखाजोखा है। रामायण काल में हो महाभारत काल, हिंसा का बोलबाला सदा से ही रहा। हिंसा के बल पर ही समाज में अनुशासन स्थापित हो पाता है।
तो फिर अहिंसा के पक्ष में इतना कुछ क्यों कहा गया है? मेरी धारणा है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक दिशा में अग्रसर होता है वह अहिंसा का मार्ग अपनाता है, भौतिक सुख छोड़ देता है, अधिकाधिक संपदा अर्जित करने से बचता है, इत्यादि। प्राचीन काल में आध्यात्मिक उत्थान को अधिक महत्व दिया जाता था र्भौतिक उन्नति की तुलना में। “अहिंसा परमो धर्मः” धर्म के उसी आध्यात्मिक पक्ष के संदर्भ में कहा गया होगा यह मेरा मत है। धर्म के इस पक्ष को आम जन व्यवहार में न तब अपना सकते थे और न अब।
हिंसा पूर्णतः त्याज्य कभी नहीं रही है। इस विषय पर किंचित् चर्चा मेरे आगामी लेख में। – योगेन्द्र जोशी


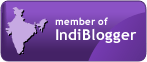

जुलाई 23, 2020 @ 10:57:18
‘तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं च कार्याकार्य व्यवस्थितौ ‘न तो पूर्ण अहिंसा से राष्ट्र का कल्याण संभव है न पूर्ण हिंसा से।पूर्ण अहिंसा राष्ट्र को संकुचित बनाती है, हिंसा राष्ट्र को बर्बर बनाती है
जुलाई 23, 2020 @ 13:19:12
मैं आपसे सहमत हूं। मैं समझता हूं कि अहिंसा की बातें व्यक्ति के आत्मिक उत्थान के लिए कही गई हैं। इसका संबंध अध्यात्म से होना चाहिए। व्यवहारिक जीवन में दुनिया शुद्ध अहिंसा से नहीं चलती।