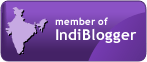महर्षि व्यासकृत महाकाव्य महाभारत में एक प्रकरण है, महाराज धृतराष्ट्र एवं ज्ञानी विदुर के मध्य संवाद का। विदुर वस्तुतः ऋषि व्यास से उत्पन्न दासीपुत्र थे और उचितानुचित की समझ रखने वाले नीतिज्ञ व्यक्ति थे। इतना और बता दूं कि प्राचीन काल में “नियोग” नामक प्रथा प्रचलित थी जिसके अंतर्गत देवर या अतिनिकट संबधी के संसर्ग से नि:संतान विधवाएं सन्तान जन्मती थीं। ऐसी सन्तान को क्षेत्रज कहा जाता था। धृतराष्ट्र एवं पांडु राजा विचित्रवीर्य की विधवा महारानियों, क्रमशः अंबिका एवं अंबालिका, से जन्मीं क्षेत्रज संतानें थीं। इस नाते विदुर धृतराष्ट्र के भाई थे। धृतराष्ट्र जब भी असमंजस या अनिर्णय की स्थिति में होते थे तो विदुर से सलाह-मशविरा करते थे।
महाभारत के उद्योग पर्व के अध्याय ३३ से ४० में विदुर द्वारा कहे गए नीति वचनों का उल्लेख मिलता है। इन अध्यायों के ग्रंथ रूप में उपलब्ध संकलन को विदुरनीति के नाम से जाना जाता है। मैं उसी ग्रंथ के प्रथम अध्याय के कुछएक श्लोकों का उल्लेख कर रहा हूं। इन छंदों में ज्ञानी विदुर “पंडित” की परिभाषा समझाते हैं।
मेरी समझ में पंडित शब्द बहुआयामी अर्थ रखता है। आम जनभाषा में किसी विषय विशेष का जानकार पंडित कहा जाता है। उसके ज्ञान को पांडित्य कहकर पुकारा जाता है। हम लोग ब्राह्मण कुल में जन्मे व्यक्ति को भी अक्सर पंडित कहते है, खास तौर पर जब वह पौरोहित्य कर्म करता हो। इस संबोधन में कदाचित यह भावना निहित रहती है कि ऐसे व्यक्ति धर्मज्ञ होगा, धर्मकर्म में लगा रहता होगा। (यद्यपि ऐसा आज के युग में होता नहीं।) विदुर इस शब्द को कई प्रकार से परिभाषित करते हैं; सभी के निचोड़ से पंडित किसे कहें यह समझा जा सकता है। विदुरनीति के प्रथम अध्याय से चयनित संबंधित छंद आगे प्रस्तुत हैं:
आत्मज्ञानं समारम्भस्तितिक्षा धर्मनित्यता ।
यमर्थान्नापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते ॥२०॥
(आत्म-ज्ञानम् समारम्भः तितिक्षा धर्म-नित्यता यम् अर्थात् न अपकर्षन्ति सः वै पंडितः उच्यते ।)
आत्मज्ञान, उद्योग, कष्ट सहने की सामर्थ्य, और धर्म में स्थिरता, ये बातें जिसको “अर्थ” से भटकाती नहीं वही पंडित कहलाता है।
इस छंद का मन्तव्य मुझे स्पष्टतः समझ में नहीं आया। मेरे विचार में आत्मज्ञान का तात्पर्य कदाचित् समाज एवं स्वयं के प्रति अपने कर्तव्यों एवं आध्यात्मिक दर्शन की समझ से होगा। उद्योग है किसी न किसी परिश्रम में स्वयं को लगाना। “अर्थ” का तात्पर्य जीवन की आवश्यकता के प्रतीक भौतिक संपदा से है। भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य का जीवन और उसकी सार्थकता चार पुरुषार्थों पर टिके हैं : धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। धर्म – कर्तव्यों का निर्वाह; अर्थ – जीवन के आधार संपदा की प्राप्ति; काम – इच्छापूर्ति यानी भोग; और मोक्ष – कामनाओं से मुक्त होकर संसार त्याग। उक्त श्लोक में उल्लिखित अर्थ इन्हीं में से एक है।
निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते ।
अनास्तिकः श्रद्दधान एतत् पण्डितलक्षणम् ॥२१॥
(निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते अ-नास्तिकः श्रद्दधानः एतत् पण्डित-लक्षणम् ।)
जो प्रशंसनीय कार्यों में लगा रहता है और निन्द्य कार्यों से दूर रहता है, जो नास्तिक नहीं है और सद्विचारों के प्रति श्रद्धालु है उसके संबंधित गुण उसके पंडित होने के लक्षण दर्शाते हैं।
नास्तिक का क्या अर्थ है? आम तौर पर नास्तिक का अर्थ ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करना समझा जाता है। लेकिन इसके अर्थ अधिक व्यापक हैं ऐसा मैं मानता हूं। ऐहिक (इस लोक के) जीवन से परे भी कुछ है इस विश्वास को आस्तिकता कहा जाएगा। जीवन के परे है क्या इसका ठीक-ठीक ज्ञान न होने पर भी “कुछ है” में विश्वास रखने वाला आस्तिक कहा जाएगा।
क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च ह्रीः स्तम्भो मान्यमानिता ।
यमर्थान्नापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते ॥२२॥
(क्रोधः हर्षः च दर्पः च ह्रीः स्तम्भः मान्य-मानिता यम् अर्थात् न अपकर्षन्ति सः वै पंडितः उच्यते ।)
क्रोध, खुशी, गर्व, लजा-भाव, उद्दंडता, स्वयं को माननीय (श्रेष्ठ) समझने का भाव, ये गुण-अवगुण जिसको पुरुषार्थ से विमुख नहीं करते उसी को पंडित कहा जाता है।
दरअसल इस परिभाषा के अनुसार जो व्यक्ति पुरुषार्थ, अर्थात् शास्त्रसम्मत कर्तव्यों, में लगा रहता है उसे न क्रोध विचलित करता है और न ही खुशी या मनुष्य स्वभाव के अन्य पहलू। स्वयं को श्रेष्ठ मानते हुए दूसरों द्वारा पूज्य माने जाने की इच्छा बहुतों को होती है, किंतु पंडित उससे मुक्त रहता है।
यस्य कृत्यं न जानन्ति मन्त्रं वा मन्त्रितं परे ।
कृतमेवास्य जानन्ति स वै पंडित उच्यते ॥२३॥
(यस्य कृत्यम् न जानन्ति मन्त्रम् वा मन्त्रितम् परे कृतम् एव अस्य जानन्ति सः वै पंडितः उच्यते)
दूसरे लोग जिसके कर्तव्य को नहीं जानते, न उसके परामर्श या जिसका विचार किया गये को, बल्कि जिसके संपन्न किए कार्य को ही केवल अन्य जन जान पाते हैं उसी को पंडित कहते हैं।
कर्तव्य से तात्पर्य यहां पर उन बातों से नहीं है जिनकी आम चर्चा मानव समाज में की जाती है, बल्कि इससे मतलब है किसी अवसर पर क्या करना उचित होगा इसका निर्णय लेना है। व्यक्ति किसी को क्या सलाह देगा, अपने मन में वह क्या विचार कर रहा है, इन बातों का ज्ञान या अनुमान दूसरों को नहीं हो पाता है। अन्य लोग उसके किए जा चुके कार्य ही केवल जान पाते हैं। असल में उक्त श्लोक में यह बताया गया है कि पंडित व्यक्ति ढिंढोरा पीटकर कार्य नहीं करता है, वह इस बात का हल्ला नहीं करता कि मैं यह करूंगा, वह करूंगा। वह बिना कुछ कहे कार्य संपन्न करता है और उस संपादित कार्य को देखकर लोगों को उसकी योजना समझ में आती है। इसके विपरीत बहुत-से लोग हल्ला अधिक मचाते हैं किंतु काम कम करते हैं।
यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः ।
समृद्धिरसमृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते ॥२४॥
(यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम् उष्णम् भयम् रतिः समृद्धिः असमृद्धिः वा सः वै पंडितः उच्यते ।)
जिसके किये जा रहे कार्य में सर्दी-गर्मी, भय, प्रेम, संपन्नता अथवा विपन्नता विघ्न नहीं डालतीं उसी को पंडित कहते हैं।
सर्दी-गर्मी आदि बातें पंडित व्यक्ति को सद्विचारों एवं सत्कर्मों से विचलित नहीं करतीं यह श्लोक का भाव है। उक्त सभी श्लोकों में व्यक्त भावों को समग्रता में देखकर ही पंडित, यानी समझदार, बुद्धिमान, विद्वान व्यक्ति को परिभाषित किया जाना चाहिए।
विदुर के द्वारा दी गई परिभाषा वस्तुतः एक आदर्श प्रस्तुत करता है। ऐसे सर्वगुणसंपन्न व्यक्ति समाज में अलभ्य ही होते हैं। फिर भी इन लक्षणों के निकट पहुंचे व्यक्ति कुछ हद तक मिल सकते हैं। – योगेन्द्र जोशी