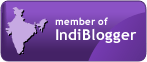समाज में धन की महत्ता सर्वत्र प्रायः सबके द्वारा स्वीकारी जाती है, और धनसंचय के माध्यम से स्वयं को सुरक्षित रखने का प्रयत्न कमोबेश सभी लोग करते हुए देखे जाते हैं । कदाचित् विरले लोग ही इस प्रश्न पर तार्किक चिंतन के साथ विचार करते होंगे कि धन की कितनी आवश्यकता किसी को सामान्यतः हो सकती है । यदि किसी मनुष्य को असीमित मात्रा में धन प्राप्त होने जा रहा हो तो क्या उसने उस पूरे धन को स्वीकार कर लेना चाहिए, या उसने इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि किस प्रयोजन से एवं किस सीमा तक उस धन के प्रति लालायित होना चाहिए । यह प्रश्न मेरे मन में वर्षों से घर किया हुए है । नीतिग्रंथों में प्राचीन भारतीय चिंतकों के एतद्संबंधित विचार पढ़ने को मिल जाते हैं । ऐसा ही एक शिक्षाप्रद एवं चर्चित ग्रंथ पंचतंत्र है । मुझे उसमें धन के बारे में गंभीर सोच देखने को मिलती है । मैं उस ग्रंथ से चुनकर दो श्लोकों को यहां पर उद्धृत कर रहा हूं:
(स्रोत: विष्णुशर्मारचित पञ्चतन्त्र, भाग 1 – मित्रसंप्राप्ति, श्लोक १५३ एवं १५४, क्रमशः)
दातव्यं भोक्तव्यं धनविषये सञ्चयो न कर्तव्यः ।
पश्येह मधुकरिणां सञ्चितमर्थं हरन्त्यन्ये ॥
(दातव्यम्, भोक्तव्यम्, धन-विषये सञ्चयः न कर्तव्यः, पश्य इह मधुकरिणाम् सञ्चितम् अर्थम् हरन्ति अन्ये ।)
अर्थः (धन का दो प्रकार से उपयोग होना चाहिए ।) धन दूसरों को दिया जाना चाहिए, अथवा उसका स्वयं भोग करना चाहिए । किंतु उसका संचय नहीं करना चाहिए । ध्यान से देखो कि मधुमक्खियों के द्वारा संचित धन अर्थात् शहद दूसरे हर ले जाते हैं ।
पंचतंत्र के रचनाकार का मत है कि मनुष्य को धन का उपभोग कर लेना चाहिए अथवा उसे जरूरतमंदों को दान में दे देना चाहिए । अवश्य ही उक्त नीतिकार इस बात को समझता होगा कि धन कमाने के तुरंत बाद ही उसका उपभोग संभव नहीं है । उसका संचय तो आवश्यक है ही, ताकि कालांतर में उसे उपयोग में लिया जा सके । उसका कहने का तात्पर्य यही होगा कि उपभोग या दान की योजना व्यक्ति के विचार में स्पष्ट होनी चाहिए । धनोपार्जन एवं तत्पश्चात् उसका संचय बिना विचार के निरर्थक है । बिना योजना के संचित वह धन न तो व्यक्ति के भोग में खर्च होगा और न ही दान में । नीतिकार ने मधुमक्खियों का उदाहरण देकर यह कहना चाहा है कि संचित धन देर-सबेर दूसरों के पास चला जाना है । मधुमक्खियों का दृष्टांत कुछ हद तक अतिशयोक्तिपूर्ण है । वे बेचारी तो शहद का संचय भविष्य में अंडों से निकले लारवाओं के लिए जमा करती हैं, जिनके विकसित होने में वह शहद भोज्य पदार्थ का कार्य करता है । यह प्रकृति द्वारा निर्धारित सुनियोजित प्रक्रिया है । किंतु उस शहद को मनुष्य अथवा अन्य जीवधारी लूट ले जाते हैं । मनुष्य के संचित धन को भले ही कोई खुल्लमखुल्ला न लूटे, फिर भी वह दूसरों के हाथ जाना ही जाना है, यदि उसे भोग या दान में न खर्चा जाए । कैसे, यह आगे स्पष्ट किया जा रहा है ।
दानं भोगं नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य ।
यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतिया गतिर्भवति ॥
(दानम्, भोगम्, नाशः, तिस्रः गतयः भवन्ति वित्तस्य, यः न ददाति, न भुङ्क्ते, तस्य तृतिया गतिः भवति ।)
अर्थः धन की संभव नियति तीन प्रकार की होती है । पहली है उसका दान, दूसरी उसका भोग, और तीसरी है उसका नाश । जो व्यक्ति उसे न किसी को देता है और न ही उसका स्वयं भोग करता है, उसके धन की तीसरी गति होती है, अर्थात् उसका नाश होना है ।
इस स्थल पर धन के ‘नाश’ शब्द की व्याख्या आवश्यक है । मेरा मानना है कि धन किसी प्रयोजन के लिए ही अर्जित किया जाना चाहिए । अगर कोई प्रयोजन ही न हो तो वह धन बेकार है । जीवन भर ऐसे धन का उपार्जन करके, उसका संचय करके और अंत तक उसकी रक्षा करते हुए व्यक्ति जब दिवंगत हो जाए तब वह धन नष्ट कहा जाना चाहिए । वह किसके काम आ रहा है, किसी के सार्थक काम में आ रहा है कि नहीं, ये बातें यह उस दिवंगत व्यक्ति के लिए कोई माने नहीं रखती हैं ।
अवश्य ही कुछ जन यह तर्क पेश करेंगे कि वह धन दिवंगत व्यक्ति के उत्तराधिकारियों के काम आएगा । तब मोटे तौर पर मैं दो स्थितियों की कल्पना करता हूं । पहली तो यह कि वे उत्तराधिकारी स्वयं धनोपार्जन में समर्थ और पर्याप्त से अधिक स्व्यमेव अर्जित संपदा का भरपूर भोग एवं दान नहीं कर पा रहे हों । तब भला वे पितरों की छोड़ी संपदा का ही क्या सदुपयोग कर पायेंगे ? उनके लिए भी वह संपदा अर्थहीन सिद्ध हो जाएगी । दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि वे उत्तराधिकारी स्वयं अयोग्य सिद्ध हो जाए और पुरखों की छोड़ी संपदा पर निर्भर करते हुए उसी के सहारे जीवन निर्वाह करें । उनमें कदाचित् यह सोच पैदा हो कि जब पुरखों ने हमारे लिए धन-संपदा छोड़ी ही है तो हम क्यों चिंता करें । सच पूछें तो इस प्रकार की कोई भी स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण एवं कष्टप्रद होगी । कोई नहीं चाहेगा कि ऐसी नौबत पैदा हो । तब अकर्मण्य वारिसों के हाथ में पहुंची संपदा नष्ट ही हो रही है यही कहा जाएगा । एक उक्ति है: “पूत सपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय ।” जिसका भावार्थ यही है कि सुपुत्र (तात्पर्य योग्य संतान से है) के लिए धन संचय अनावश्यक है, और कुपुत्र (अयोग्य संतान) के लिए भी ऐसा धन छोड़ जाना अंततः व्यर्थ सिद्ध होना है ।
कुल मिलाकर पंचतंत्र के रचयिता के मतानुसार धन का भोग और दान करने के बजाय महज उसका संचय करते रहना उसके नाश के तुल्य ही है । – योगेन्द्र जोशी