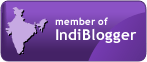निकट भविष्य में देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। अपने-अपने हित साधने या अस्तित्व बचाने के लिए राजनैतिक दल मेल-बेमेल गठबंधन बनाने में जुटे हैं। बेमेल गठबंधनों को देखने पर मुझे महाकाव्य महाभारत (शान्ति पर्व, अध्याय १३८) में वर्णित विडाल (बिलाव) एवं मूषक (मूस) की अल्पकालिक मित्रता की एक कथा याद आ रही है। उसी कथा से संबंधित कुछएक नीतिवचनों का उल्लेख यहां पर कर रहा हूं।
संक्षेप में कथा कुछ इस प्रकार है — किसी वन में एक विशाल पेड़ था, जिसके जड़ के पास एक मूस (बड़े आकार का चूहा) बिल बनाकर रहता था। उसी पेड़ पर एक बिलाव (बिल्ला) भी रहा करता था। बिल्ले से बचते हुए मूस बिल के बाहर भोजन की तलाश में निकला करता था।
एक बार एक बहेलिये ने पेड़ के पास जाल बिछा दिया, जंगली जानवरों एवं पक्षियों को फंसाकर कब्जे में लेने के लिए। उसका इरादा दूसरे दिन प्रातः आकर उन पशु-पक्षियों को ले जाने का था जो जाल में फंसे हों। दुर्भाग्य से वह बिलाव जाल में फंस गया। उसे जाल में फंसा देख चूहा आश्वस्त हो गया और निर्भय होकर इधर-उधर भोजन तलाशने लगा। कुछ देर में उसे एक नेवला दिखाई दिया जो उस मूस की गंध पाकर उस स्थान के आसपास पहुंचा और उसे मारने के लिए मौके का इंतिजार करने लगा। मूस को पेड़ की एक डाल पर बैठा हुआ एक और दुश्मन उल्लू भी नजर आया। मूस को तीन-तीन शत्रु आसपास नजर आए।
वस्तुस्थिति को देख उसने सोचा, “अपने बिल की ओर जाना अभी मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। तीनों शत्रुओं में मेरा सबसे बड़ा शत्रु, जिससे शेष दो भी दूरी बनाए रखते हैं, जाल में फंसा असहाय है। अपनी खुद की विवशता देख मुझे मारने का प्रयास नहीं करेगा। अतः उसी के सान्निध्य में पहुंचकर अपने को सुरक्षित रखना बुद्धिमत्ता होगी। उसकी सुरक्षा का आश्वासन देकर मैं स्वयं उसका विश्वास पा सकता हूं।”
उसने बिल्ले के पास जाकर कहा, “मित्र बिडाल, आप इस समय आपत्ति में फंसे हैं। जाल काटकर मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, बशर्ते आप मेरी सुरक्षा के लिए बचनबद्ध होवें।”
बिल्ले ने कहा, “ठीक है मुझे मंजूर है। परन्तु मुझे करना क्या है?”
“आप मुझे अपने संरक्षण में ले लें ताकि मैं सुरक्षित रात बिता सकूं। मैं आपको वचन देता हूं कि प्रातः बहेलिये के आने तक मैं आपको पाश-मुक्त कर दूंगा।” मूस ने कहा।
बिल्ले ने उसकी बात मान ली। उसने समझ लिया था कि उस परिस्थिति में कोई उसे बचाने नहीं आने वाला। मूस ही उसका हित साध सकता था, इसलिए उसकी बात मानना उसकी मजबूरी बन चुकी थी। इसके बाद वह बीच-बीच में मूस को उसके वचन की याद दिलाता और पूछता कि वह कब उसके बंधन काटेगा। प्रातःकाल होते-होते मूस ने जाल के कई तंतुओं को काट लिए, लेकिन कुछ बंधन जानबूझकर छोड़े रखा।
बिल्ला उसको याद दिला रहा था कि जब उन दोनों ने परस्पर मित्रता कर ली है तो वह जाल के बंधन काटकर उसे मुक्त क्यों नहीं कर रहा है। तब मूस ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए बिल्ले को ये नीतिवचन सुनाए:
न कश्चित्कस्यचिन्मित्रं न कश्चित्कस्यचिद् रिपु: ।
अर्थतस्तु निबध्यन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥११०॥
(महाभारत, शान्तिपर्व के अंतर्गत आपद्धर्मपर्व, अध्याय १३८)
(कश्चित् कस्यचित् मित्रम् न, कश्चित् कस्यचित् रिपु: न, मित्राणि तथा रिपवः अर्थत: तु निबध्यन्ते ।)
अर्थ – न कोई किसी का मित्र होता है और न ही शत्रु। अपने-अपने स्वार्थवश ही मित्र तथा शत्रु परस्पर जुड़ते हैं। [वैकल्पिक अर्थ – मनुष्य से जुड़ते हैं।]
और
शत्रुरूपा हि सुहृदो मित्ररूपाश्च शत्रवः ।
संधितास्ते न बुध्यन्ते कामक्रोधवशं गताः ॥१३८॥
(यथा उपर्युक्त)
(सुहृदः शत्रुरूपाः हि शत्रवः च मित्ररूपाः, संधिताः ते काम-क्रोध-वशं गताः न बुध्यन्ते ।)
अर्थ – परिस्थिति के अनुरूप सुहृज्जन भी शत्रुरूप धारण कर लेते हैं (शत्रु बन जाते हैं) और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। परस्पर संधि (समझौते) से जुड़े होने पर भी काम (प्रबल इच्छा) एवं क्रोध के वशीभूत होने पर (उनके व्यवहार से) समझ में नहीं आता कि वे शत्रु हैं या मित्र?
उक्त दो छंदों के माध्यम से चूहे ने यह स्पष्ट किया कि मित्रता एवं शत्रुता का आधार स्वार्थ होता है। फलतः परिस्थितियां बदल जाने पर मित्रता-शत्रुता के भाव भी बदल जाते हैं। परस्पर मित्रता से बंधे होने पर भी जब व्यक्ति के मन में प्रबल इच्छा-भाव जगता है या उसे आक्रोश घेर लेता है मित्रता का विचार बदल जाता है।
मूस के कहने का मंतव्य यह है कि जब दो जने मित्रता में बंधे होते हैं तब भी विपरीत परिस्थिति पैदा हो जाने पर अपनी प्रबल इच्छा अथवा गुस्सा के वशीभूत होने पर वे मित्रता का भी ध्यान खो बैठते हैं। उसने स्पष्ट संकेत बिल्ले को दिया कि यदि वह जाल से मुक्त हो गया तो वह मित्रता का वचन भुला सकता है और उसी (मूस) पर हमला कर सकता है। इसलिए वह उसे (बिल्ले को) को मुक्त करने को उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करेगा।
आगे मूस इस तथ्य की ओर ध्यान खींचता है कि
नास्ति मैत्री स्थिरा नाम न च ध्रुवमसौहृदम् ।
अर्थयुक्त्यानुजायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥१४१॥
(यथा उपर्युक्त)
(मैत्री नाम स्थिरा न अस्ति, असौहृदम् च न ध्रुवम्, मित्राणि तथा रिपवः अर्थ-युक्त्या अनुजायन्ते ।)
अर्थ – अवश्य ही मित्रता स्थायी नहीं होती और विद्वेष भी स्थायी नहीं होता। स्वार्थ से(अर्थात् अपने-अपने हित साधने के लिए) ही लोग मित्र एवं शत्रु बनते हैं।
कहने का तात्पर्य यह है कि मित्रता एवं शत्रुता मौके-मौके की बातें है। जब व्यक्ति को किसी से अपने स्वार्थ सिद्ध करने हों तो वह मित्रता कर लेता है। किन्तु जब उनके हित टकराने लगते हैं तो वह व्यक्ति शत्रुता पर उतर आता है। उसने बिलाव को याद दिलाया कि उन दोनों की मित्रता अस्थायी है और कभी भी टूट सकती है।
मूस के अनुसार हमारे सामाजिक रिश्ते दरअसल स्थार्थ्यजनित ही होते हैं जैसा अगले छंद में कहा गया है:
अर्थयुक्त्या हि जायन्ते पिता माता सुतस्तथा ।
मातुला भागिनेयाश्च तथासम्बन्धिबान्धवाः ॥१४५॥
(यथा उपर्युक्त)
(पिता माता सुत: तथा च मातुलाः भागिनेया: तथा सम्बन्धि-बान्धवाः अर्थ-युक्त्या हि जायन्ते ।)
अर्थ – माता, पिता, पुत्र, मामा, भांजा इत्यादि संबंधी एवं बंधुबान्धव आदि के परस्पर संबंध स्वार्थ के कारण बनते हैं।
स्वार्थ में कितनी शक्ति है यह अगले नीति-छंद से स्पष्ट होता है:
पुत्रं हि मातापितरौ त्यजतः पतितं प्रियम् ।
लोको रक्षति चात्मानं पश्य स्वार्थस्य सारताम् ॥१४६॥
(यथा उपर्युक्त)
(पतितम् प्रियम् पुत्रं हि माता-पितरौ त्यजतः, लोक: रक्षति च आत्मानम् स्वार्थस्य सारताम् पश्य ।)
अर्थ –मार्गभ्रष्ट (चारित्रिक तौर से गिरे) पुत्र (संतान) को माता-पिता भी त्याग देते हैं। निश्चय ही मनुष्य पहले अपनी रक्षा करता है। देखो स्वार्थ का सार इसी तथ्य में निहित है।
अर्थात् यदि संतान के कारण अपनी प्रतिष्ठा गिरने का डर हो तब माता-पिता भी उसका बहिष्कार कर डालते हैं। ऐसा कुछ आज के समाज में देखने को कम ही मिलता है। इस युग में बहिष्कार-योग्य व्यक्ति का बचाव करने माता-पिता ही नहीं अपितु संबंधी, परिचित, मित्र आदि भी मैदान में कूद पड़ते हैं। शायद प्राचीन काल में कभी स्थिति भिन्न रही होगी।
इन नीति-वचनों के द्वारा मूस स्पष्ट कर देता है कि वह बिलाव की मित्रता के प्रति पूर्णतः आश्वस्त नहीं हो सकता है।
इस कथा का अंत इस प्रकार है — प्रातःकाल मूस एवं बिलाव बहेलिये को निकट आता हुए दिखते हैं। तब सही क्षण पर मूस अपना वचन निभाते हुए जाल के शेष बंधन काटकर बिलाव को बंधन-मुक्त कर देता है और तेजी से अपने बिल की ओर भाग जाता है। बिलाव भी बहेलिए को पास आ चुका देखकर पेड़ की ओर भागकर उसमें चढ़ जाता है। इसके साथ ही उन दोनों के बीच की अल्पकालिक मित्रता समाप्त हो जाती है।
इस स्थल पर एक टिप्पणी करना समीचीन होगा। प्राचीन संस्कृत साहित्य में शिक्षाप्रद संदेश देने के ऐसे दृष्टांत देखने को मिल जाते हैं जिनमें पशु-पक्षियों को पात्रों के तौर पर प्रयोग में लिया गया हो। पंचतंत्र एवं हितोपदेश ऐसी शैली या परंपरा के सुविख्यात उदाहरण हैं। महाभारत महाकाव्य ग्रंथ में भी किसी-किसी स्थल पर पशु-पक्षियों के माध्यम से दिए गए नीति संदेश पढ़ने को मिल जाते हैं। इस विधि से दिए गए नीति-संदेश मनोरंजक होते हैं न कि शुष्क एवं उबाऊ। – योगेन्द्र जोशी