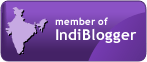पंचतंत्र के नीतिवचनों पर आधारित अपनी 7 फरवरी 2010 की पोस्ट में मैंने ग्रंथ का संक्षिप्त और एक प्रकार से अधूरा परिचय दिया था। उसके बारे में इस स्थल पर विस्तार से बताना मेरा उद्देश्य नहीं है। फिर भी इतना कहना चाहूंगा कि इसमें व्यावहारिक जीवन से संबंधित सार्थक नीति की तमाम बातें कथाओं के माध्यम से समझाई गयी हैं । इन कथाओं में अधिकतर पात्र मनुष्येतर प्राणी यथा लोमड़ी, शेर, बैल, कौआ आदि हैं। कथाएं आपस में शृंखलाबद्ध तरीके जुड़ी हुई हैं अर्थात् एक कथा में दूसरी कथा और उसमें तीसरी आदि के क्रम से कथाओं का बखान किया गया है। उक्त ग्रंथ पांच खंडों में विभक्त है जिन्हें “तंत्र” पुकारा गया है। ये हैं:
1. मित्रभेदः, 2. मित्रसंप्राप्तिः, 3. काकोलूकीयम्, 4. लब्धप्रणाशम्, एवं 5. अपरीक्षितकारकम् ।
प्रत्येक तंत्र में किसी एक प्रकार की विषयवस्तु लेकर कथाएं रची गई हैं, जैसे मित्रभेदः में वे कथाएं हैं जो दिखाती हैं कि किस प्रकार प्रगाढ़ मित्रों के बीच फूट डालकर अपना हित साधा जा सकता है। इसी प्रकार अंतिम तंत्र अपरीक्षितकारकम् में वे कथाएं हैं जो दर्शाती हैं कि समुचित सोचविचार के बिना किया जाने वाला कार्य कैसे घातक हो सकता है।
पंचतन्त्र का आरंभ कुछ यों होता है: सुना जाता है कि दक्षिण देश में महिलारोप्य नामक नगर हुआ करता था। वहां अमरशक्ति नाम के हर प्रकार से योग्य राजा शासन करते थे। उनके तीन पुत्र थे जिनके नाम क्रमश: बहुशक्ति, उग्रशक्ति तथा अनंतशक्ति थे। कुबुद्धि प्रकार के वे तीनों राजपुत्र शास्त्रादि के अध्ययन में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते थे। राजा उनके बारे में सोच-सोचकर दुःखी रहते थे। उन्होंने एक बार अपने मन के बोझ की बात मंत्रियों के सामने रखते हुए राजपुत्रों को विवेकशील एवं शिक्षित बनाने के उपाय के बारे में पूछा। सोचविचार के बाद मंत्रियों ने उन्हें बताया कि शास्त्रों एवं अनेक विद्याओं के ज्ञाता एक ब्राह्मण राज्य में हैं। उन्हीं के संरक्षण में राजपुत्रों को सौंप दिया जाए। ब्राह्मण ने राजपुत्रों को सुधारने का जिम्मा ले लिया इस शर्त के साथ कि वे छः महीने तक उनके साथ रहेंगे और राजा या अन्य कोई उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये ब्राह्मण स्वयं पंचतंत्र ग्रंथ के रचयिता विष्णुशर्मा थे। माना जा सकता है कि विष्णुशर्मा ने सरल, रोचक, एवं शिक्षाप्रद कथाओं के माध्यम से राजपुत्रों में विद्याध्ययन के प्रति रुचि जगाई।
मैं यहां पर उक्त ग्रंथ की एक कथा प्रस्तुत करते हुए नीतिप्रद श्लोकों का उल्लेख कर रहा हूं।
एक बार एक बहेलिये ने पक्षियों को पकड़ने के लिए जंगल में चारा डालते हुए जाल फैला दिया। कुछ समय बाद कबूतरों का एक झुंड उधर आया और वहां पड़े चारे को खाने के लिए लालायित हुआ। कबूतरों के मुखिया/राजा, चित्रग्रीव, ने झुंड के सदस्यों से कहा, “इतना सारा चारा यहां पर कैसे और कहां से आया होगा यह सोचने की बात है। अवश्य ही कुछ रहस्य है और हमें इससे बचना चाहिए।”
झुंड के सदस्यों ने कहा, “आप यों ही सशंकित हो रहे हैं। इसे चुगने पर कोई खतरा नहीं होगा।” और वे सभी नीचे उतर गए और जाल में फंस गए।
स्वयं को विपत्ति में पड़ा हुआ पाने पर कतोतराज चित्रग्रीव ने शेष कबूतरों से कहा, “तुम लोग धैर्य से काम लेना। अब हम एक कार्य कर सकते हैं। जाल समेत यहां से उड़ चलें और हिरण्यक नामक मेरे घनिष्ठ मित्र चूहे के पास पहुंचें। वह जंगल ही में एक पेड़ के जड़ के पास बने बिल में रहता है।”
उस पेड़ के पास पहुंचने पर चित्रग्रीव ने मित्र हिरण्यक चूहे को मदद के लिए पुकारा। हिरण्यक ने जानी-पहचानी सी आवाज सुनी तो उसने बिल के अंदर से ही पूछा, “कौन है बाहर मुझे पुकारने वाला? नाम-पता तो बताओ।”
चित्रग्रीव ने जवाब दिया, “भाई, मैं हूं तुम्हारा मित्र कपोतराज चित्रग्रीव। मैं विपत्ति में फंस गया हूं, इसलिए शीघ्र मेरी मदद करो।”
हिरण्यक ने बिल से बाहर निकलने पर देखा कि उसका मित्र अपने साथी कबूतरों के साथ जाल में फंसा हुआ है। वह शीघ्र चित्रग्रीव के पास पहुंचा और उसके बंधन काटने लगा। कपोतराज ने उसे मना किया और कहा, “पहले इनके बंधन काटो और अंत में मेरे।”
हिरण्यक ने आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा, “पहले तुम्हें मुक्त होना चाहिए। बाद में देर हो जाए, या मैं थक जाऊं, अथवा मेरे दांत टूट जाएं तो तुम्हें मुक्त करना संभव नहीं हो पाएगा।”
“मैं इन सब का मुखिया हूं, राजा हूं। मेरा कर्तव्य है कि पहले प्रजा का हित साधूं न कि अपना। मुझे त्याग करना पड़े तो कोई बात नहीं; इनकी मुक्ति पहले होनी चाहिए।” कपोतराज ने उत्तर दिया।
हिरण्यक ने सहमति जताते हुए कहा, “मित्र, मैं तो देखना चाहता था कि तुम राजा के तौर पर कितने स्वार्थी हो। मुझे विश्वास था ही तुम योग्य राजा के अनुरूप ही निर्णय लोगे।” और उसने तेजी से उन सभी के बंधन काट डाले। तब दोनों मित्रों के बीच कर्तव्याकर्तव्य और कुशलक्षेम की संक्षिप्त बातें हुई और अंत में चित्रग्रीव ने हिरण्यक के प्रति आभार प्रकट करते हुए विदा ली। हिरण्यक भी सतर्क अपने बिल में सुरक्षित चला गया।
उसी पेड़ की एक डाली पर लघुपतनक नामक एक कौआ भी रहता था। वह उस घटना को देख रहा था और दोनों के बीच हुए वार्तालाप को ध्यान से सुन रहा था। चूहे हिरण्यक की विद्वतापूर्ण बातें उसे खूब भाईं और उसे लगा कि उससे मित्रता की जानी चाहिए। तब वह बिल के पास आकर बोला, “अरे हिरण्यक भाई, बाहर आओ, मैं भी तुमसे मित्रता करना चाहता हूं।”
हिरण्यक ने उससे उसका परिचय जानना चाहा। उस कौवे ने बताया कि वह लघुपतनक नाम का कौआ है जो उसी पेड़ पर रहता है। अपने बिल में सुरक्षित टिके हुए हाजिरजवाब हिरण्यक ने आपत्ति जाहिर की, “अरे काक लघुपतनक, तुम्हारे-मेरे मध्य मित्रता कैसे संभव है? मेरी प्रजाति तो तुम्हारी प्रजाति के लिए भक्ष्य है। मैं शिकार और तुम शिकारी। मैं तो तुम्हारी मौजूदगी में बिल के बाहर भी निकलने की हिम्मत नहीं सकता, दोस्ती तो बहुत दूर की बात है।”
हिरण्यक ने बिल के अंदर से ही लघुपतनक से कहा कि परस्पर संबंध स्थापित करते समय दो जनों को अधोलिखित नीति-श्लोक पर ध्यान देना चाहिए:
ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं कुलम् ।
तयोर्मैत्री विवाहश्च न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥२९॥
(पञ्चतंत्र, द्वितीय तंत्र मित्रसंप्राप्ति)
(ययोः एव समम् वित्तम् ययोः एव समम् कुलम् तयोः मैत्री विवाहः च न तु पुष्ट-विपुष्टयोः ।)
शब्दार्थ – जिनका (दो व्यक्तियों का) समान वित्त हो, जिनका कुल समान हो, उन्हीं में परस्पर मित्रता एवं विवाह ठीक है न कि सक्षम एवं असक्षम के बीच।
अर्थात् दो जनों के मध्य यारी-दोस्ती और वैवाहिक संबंध तभी स्थापित होने चाहिए जब वे समकक्ष कुलों से जुड़े हों और उनकी आर्थिक-सामाजिक स्थिति में समानता हो। जहां दोनों के बीच आर्थिक असमानता हो या दोनों की सामाजिक प्रतिष्ठा के स्तर में अंतर हो वहां संबंध नहीं बनाए जाने चाहिए।
इसके आगे भी हिरण्यक समझाया:
यो मित्रं कुरुते मूढ आत्मनोऽसदृशं कुधीः ।
हीनं वाप्यधिकं वापि हास्यतां यात्यसौ जनः ॥३०॥
(यथा उपर्युक्त)
यः मित्रम् कुरुते मूढः आत्मनः असदृशम् कुधीः हीनम् वा अपि अधिकम् वा अपि हास्यताम् याति असौ जनः ।)
शब्दार्थ – जो कुबुद्धि अपने असमान, अपने से हीनतर हो अथवा श्रेष्ठतर, के साथ मित्रता करता है वह जगहंसाई का पात्र बन जाता है।
जो व्यक्ति अपने से सर्वथा भिन्न आर्थिक अथवा सामाजिक स्तर के व्यक्ति के साथ मित्रता अथवा पारिवारिक संबंध स्थापित करता है वह मूर्ख कहा जाएगा। ऐसा व्यक्ति अपने से श्रेष्टतर स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा हेय दृष्टि से देखा जाता है। मानव समाज में ऐसा सदैव नहीं देखने को मिलता है जहां दो, विशेषतः जब जने वैचारिक कारणों से मित्र बनते हैं। किंतु वैवाहिक मामलों में यह काफी हद तक सही है। हीनतर स्थिति वाले व्यक्ति का कभी-कभी स्पष्ट तौर पर तिरस्कार होता है। ऐसी संभावनाओं के कारण ही बराबरी के रिश्ते को उचित माना जाता है।
नीति की इस प्रकार की बातों से लघुपतनक हिरण्यक से बहुत प्रभावित हुआ। उसने समझाने की कोशिश की, “मैं तुम्हें धोखा देने के विचार से मित्रता की बात नहीं करता। मैं वास्तव में गंभीर हूं क्योंकि मैं तुमसे विद्वता की बातें सुनना चाहता हूं, तुम्हारे साथ विचारों का आदान-प्रदान करना चाहता हूं। तुम मेरा विश्वास करो।”
विश्वास की बात पर हिरण्यक ने उत्तर दिया:
न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्तेऽपि न विश्वसेत् ।
विश्वासाद्भयमुत्पन्नं मूलान्यपि निकृतन्ति ॥४४॥
(यथा उपर्युक्त)
(न विश्वसेत् अविश्वस्ते विश्वस्ते अपि न विश्वसेत् विश्वासात् भयम् उत्पन्नम् मूलानि अपि निकृतन्ति ।)
शब्दार्थ – अविश्वसनीय व्यक्ति का तो विश्वास न ही करे और विश्वसनीय पर भी विश्वास न करे। विश्वास करने पर जो संकट पैदा होता है वह जड़ों को भी काट डालता है। तात्पर्य यह कि अपने विश्वस्त पर भी पूरा विश्वास नहीं ही होना चाहिए क्योंकि वह भी धोखा दे सकता है।
न वध्यते ह्यविश्वस्तो दुर्बलोऽपि बलोत्कटैः ।
विश्वस्ताश्चाशु बध्यन्ते बलवन्तोऽपि दुर्बलैः ॥४५॥
(यथा उपर्युक्त)
(न वध्यते हि अविश्वस्तः दुर्बलः अपि बल-उत्कटैः विश्वस्ताः च आशु बध्यन्ते बलवन्तः अपि दुर्बलैः ।)
शब्दार्थ – विश्वास न हो जिसे (अविश्वस्त) ऐसा दुर्बल व्यक्ति बलशाली द्वारा भी नहीं मारा जाता है। विश्वस्त व्यक्ति तो दुर्बल के द्वारा भी शीघ्र मारा जाता है।
इन दो छंदों का उल्लेख अपनी टिप्पणी के साथ मैंने २०१० की एक प्रविष्टि (७ फरवरी) में किया है। अतः यहां पर उस टिप्पणी का पुनरुल्लेख नहीं कर रहा हूं।
टिप्पणी – उपर्युक्त छंद ४४ में द्वितीय चरण का पाठ “विश्वस्तेऽपि न विश्वसेत्” है। मेरे पास पंचतंत्र की चौखंबा विद्याभवन द्वारा प्रकाशित (वाराणसी, १९९४) की प्रति है। उसमें यही पाठ है। मुझे लगता है कि इसके बदले “विश्वस्ते नाति विश्वसेत्” होता तो अधिक उपयुक्त होता। उस स्थिति में उसका अर्थ अधिक स्वीकार्य होता। अर्थ होता “विश्वस्त व्यक्ति पर भी अधिक विश्वास नही करना चाहिए।” यानी उस पर भी थोड़ी-बहुत शंका बनी रहनी चाहिए। हो सकता है किसी अन्य संस्करण में ऐसा ही हो।
हिरण्यक को विश्वास दिलाने का लघुपतनक ने काफी प्रयास किया । उसने, “ठीक है, तुम्हें विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मित्रता न करो न सही। फिर भी अपने बिल में सुरक्षित अनुभव करते हुए मुझसे बातें तो कर ही सकते हो। मैं रोज तुम्हारी पांडित्य भरी बातें सुनने आया करूंगा, इतना तो कर सकते हो न?”
हिरण्यक ने उसकी बात मान ली। इसके बाद उन दोनों के बीच प्रायः प्रतिदिन मुलाकातें होने लगीं, पहला बिल के अंदर मुहाने पर सुरक्षित और दूसरा बिल के बाहर। दोनों के बीच विविध विषयों पर वार्तालापों का सिलसिला चल पड़ा । हिरण्यक के मन में शनैः-शनैः लघुपतनक के प्रति विश्वास एवं लगाव जगने लगा। लघुपत्तनक दिन के समय बीन-बटोर कर लाई गईं भोज्य वस्तुएं हिरण्यक को भेंट करने लगा और इसी प्रकार हिरण्यक भी रात में खोज-बीन कर लाईं चीजें लघुपतनक को खिलाने लगा। इस प्रकार के लंबे सान्निध्य के बाद हिरण्यक को लगने लगा कि लघुपतक उसे धोखा नहीं देगा। वह बिल के बाहर आने लगा। दोनों की मित्रता हो जाती है। साथ-साथ उठना-बैठना, खेलना-कूदना होने लगा।
यह है पंचतंत्र के दूसरे तंत्र, मित्रसंप्राप्ति, की एक कथा। उक्त कहानी यही पर खत्म नहीं होती। कथा के दोनों पात्र मित्र बन जाते हैं कालांतर में वे उस स्थान को छोड़कर एक नए मित्र कछुए के पास पहुंचते हैं और वहां जुड़ती है एक और कथा। और यह सिलसिला आगे बढ़ता है। – योगेन्द्र जोशी