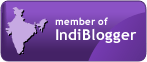इधर दो-चार दिनों से ‘सत्यम’ नामक सॉफ्टवेयर कंपनी समाचार माघ्यमों का विषय बना हुआ है, किसी सार्थक उपलब्धि के कारण नहीं, बल्कि अरबों रुपयों के घोटाले के कारण । कंपनी के अघ्यक्ष पर सब की नजर है कि कैसे उन्होंने अमीरी की सीमा रातों-रात कहीं आगे बढ़ा लेने की लालसा में एक जबरदस्त घोटाला कर डाला । इस घटना की खबर ने मेरा ध्यान इन सूक्तियों की ओर खींच डाला:
सुमहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्तो बहुश्रुताः ।
छेत्तारः संशयानां च क्लिश्यन्ते लोभमोहिताः ।। 26 ।।
लोभात्क्रोधः प्रभवति लोभात्कामः प्रजायते ।
लोभान्मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम् ।। 27 ।।
(नारायणपण्डितसंगृहीत हितोपदेश)
(अनेकों शास्त्रों का ज्ञाता तथा श्रोता, समस्याओं-शंकाओं के समाधान में निपुण पंडित भी लोभ-लालच के वशीभूत होकर क्लेश यानी कष्ट की अवस्था को प्राप्त हो जाता है । लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से कामना, यानी और अधिक अर्जित करने की इच्छा, जागृत होती है, लोभ से व्यक्ति मोह या भ्रम में पड़ता है, और उसी से विनाश की स्थिति पैदा होती है; वस्तुतः लोभ पाप का कारण है ।)
मैं समझता हूं कि लोभ करना और अधिकाधिक भौतिक संपदा बटोरना मनुष्य की निसर्ग से जन्मी स्वाभाविक वृत्ति है । उससे मुक्त होने के लिए मनुष्य को तप का सहारा लेना पड़ता है, अर्थात् आत्मसंयम का भाव मन में लाना होता है । धन-संपदा मानव समाज में सदा से ही महत्त्वपूर्ण रहे हैं, किंतु मनीषियों एवं विचारकों ने सदा ही समाज को उसकी सीमा निर्धारित करने का उपदेश दिया है । ‘अति सर्वत्र वर्जितम्’ उनके द्वारा प्रचारित नीति रही है । किसी व्यक्ति को कितना चाहिए इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए और उसी के अनुसार धन कमाने का प्रयास करना चाहिए और अति नहीं करनी चाहिए ।
पूर्व काल में लोग धन-संपदा को आवश्यक मानते थे, लेकिन उसे ही सब कुछ मान के नहीं बैठ जाते थे । एक समय था जब लोग अपने समस्त समय, ऊर्जा और बुद्धि का उपयोग केवल धनोपार्जन के लिए नहीं करते थे । धन कमाते समय वे समाज के हित-अहित के प्रति उदासीन नहीं हो जाते थे । लोगों के लिए ज्ञानार्जन, अध्यात्म, दर्शन, धार्मिक कृत्य समाज सेवा और सांस्कृतिक कार्य आदि का भी महत्त्व होता था । किंतु आज हम ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां जीवन का सर्वप्रथम लक्ष्य – और कभी-कभी एकमेव लक्ष्य – धनोपार्जन रह गया है । रातदिन यह चिंता बनी रहती है कि कैसे अधिकाधिक धन-संपदा जुटायी जाये । आज का मानव जीवन प्रतिस्पर्धात्मक बन चुका है । वह अपनी भौतिक संपदा की तुलना अन्य लोगों से अधिक करता है और इस भावना के साथ संतुष्ट नहीं हो पाता है कि उसकी आवश्यकताएं तो पूरी हो रही हैं, दूसरे से क्या तुलना करना । उसकी लालसा रहती है कि वह संपदा के मामले में अपने रिश्तेदारों, मित्र-परिचितों, पड़ोसियों, एवं सहकर्मियों आदि से आगे निकल जाये । तुलना के अन्य आधारों की कोई अहमियत आज के युग में नहीं है । हर कोई ईमानदारी, परोपकार, जनसेवा, निष्ठापूर्वक दायित्व-निर्वाह आदि में आगे रहने को मुर्खता मानता है । सादगी का जीवन तो विवशता से जोड़ा जाता है । धन को लेकर मानव-मन इतना उत्साहित है कि अपने पास जो भी खूबी हो उसे बाजार में उतारने को तैयार है । किसी व्यवसाय की महत्ता उससे जुड़े आर्थिक लाभ से आंकी जाती है । जब शारीरिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ज्ञान तक बिकाऊ हो सकते हैं तो फिर बचता क्या है ? दूसरों द्वारा लगाये गये मिथ्या लांछनों तक की भरपायी धन से संभव है । हर चीज की कीमत पैसा ! ऐसे धन के प्रति आकर्षण स्वाभाविक ही है । मुझे राजा एवं कवि भर्तृहरि के ये वचन याद आ रहे हैं:
यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पण्डितः स श्रुतवान् गुणज्ञः ।
स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति ।। 41 ।।
(भर्तृहरिविरचित नीतिशतकम्)
(जिसके पास धन है वही उच्च कुल का है, वही जानकार पंडित है, वही शास्त्रों का ज्ञाता है, वही दूसरों के गुणों का आकलन करते की योग्यता रखता है, वही प्रभावी वक्ता है, उसी का व्यक्तित्व दर्शनीय है । यह सब इसलिए कि सभी गुण धन के प्रतीक कांचन अर्थात् सोने पर निर्भर हैं । धन है तो वे गुण भी हैं, अन्यथा वे भी नहीं हैं ।)
वस्तुतः धन के बल पर ऐसे लोग जुटाये जा सकते हैं जो किसी भी व्यक्ति को ऊपर कही बातों के योग्य मानने को तैयार हों और फलतः वह व्यक्ति अयोग्य होते हुए भी सबसे आगे सिद्ध हो जाये । मैं समझता हूं कि राजा भर्तृहरि के काल में धन की इतनी महत्ता नहीं रही होगी और उपर्युक्त बातें उन्होंने एक व्यंग के तौर पर कही होंगी । परंतु आज तो धन ही सब कुछ प्रतीत होता है !– योगेन्द्र