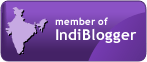“कौटिलीय अर्थशास्त्र” महान राजनीतिवेत्ता कौटिल्य द्वारा राज्य का शासन कारगर तरीके से चलाने की प्रणाली पर रचित ग्रंथ है । कौटिल्य चाणक्य (चणक-पुत्र, असल नाम विष्णुगुप्त) का वैकल्पिक नाम है, जिन्होंने करीब ढाई हजार साल पहले चंद्रगुप्त को राजगदी पर बिठाकर मौर्य राज्य की स्थापना की थी । उनके बारे में कुछ जानकारी मैंने अपने 23 सितंबर, 2009, की ब्लॉग-प्रविष्टि में दी है ।
उक्त ग्रंथ में शासकीय व्यवस्था की तमाम बातों के साथ पुरुषार्थ की महत्ता की भी बात की गई है । चाणक्य के अनुसार भाग्य के भरोसे बैठना नासमझों का काम है । ग्रंथकार ने यह भी कहा है कि धन से ही और अधिक धन का उपार्जन होता है । तत्संबंधित दो श्लोक मुझे ग्रंथ में पढ़ने को मिले हैं जिनका उल्लेख मैं इस स्थल पर कर रहा हूं ।
(स्रोत संदर्भ – कौटिलीय अर्थशास्त्र, अधिकरण 9, प्रकरण 142)
नक्षत्रमतिपृच्छन्तं बालमर्थोऽतिवर्तते ।
अर्थो ह्यर्थस्य नक्षत्रं किं करिस्यन्ति तारकाः ॥
( नक्षत्रम् अति-पृच्छन्तम् बालम् अर्थः अति-वर्तते, अर्थः हि अर्थस्य नक्षत्रम् तारकाः किम् करिस्यन्ति ।)
अर्थ – नक्षत्रों की गणना करने वाले नासमझ से धन दूर ही रहता है । दरअसल धन के लिए धन ही नक्षत्र होता है, उसके लिए तारागण की क्या भूमिका ?
धनोपार्जन के कार्य में ग्रह-नक्षत्रों की गणना, ज्योतिषीय सलाह-मशविरा, शुभ मुहूर्त का विचार, आदि का कोई महत्व नहीं होता । जो इन पचड़ों में रहता है वह व्यावहारिक जीवन में एक नादान बच्चे की-सी नासमझी करता है । असल तथ्य तो यह है कि धनोपार्जन के लिए आपके पास की धन-संपदा ही ग्रह-नक्षत्र की भूमिका निभाती हैं । तात्पर्य यह है कि आकाशीय पिंड धनोपार्जन को प्रभावित करने की क्षमता नहीं रख्रते, बल्कि आपकी पहले से ही अर्जित धनसंपदा उनकी जगह प्रभावी होती हैं, जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट है ।
नाधनाः प्राप्नुवन्त्यर्थान्नरा यत्नशतैरपि ।
अर्थैरर्थाः प्रबध्यन्ते गजाः प्रतिगजैरिव ॥
(अधनाः नराः यत्न-शतैः अपि अर्थान् न प्राप्नुवन्ति, प्रति-गजैः गजाः इव अर्थाः अर्थैः प्रबध्यन्ते ।)
अर्थ – निर्धन जन सौ प्रयत्न कर लें तो भी धन नहीं कमा सकते हैं । जैसे हाथियों के माध्यम से हाथी वश में किए जाते हैं वैसे ही धन से धन को कब्जे में लिया जाता है ।
यह सुविख्यात है कि वनक्षेत्र में रह रहे हाथी को पालतू हाथियों की मदद से वश में किया जाता है और कालांतर में उसे पालतू बनाने में सफलता मिल जाती है । कुछ ऐसा ही धन के साथ होता है । एक कहावत हैः “पैसा पैसे को खींचता है ।” जिसके निहितार्थ यही हैं । दरअसल जब मनुष्य के पास धन होता है तभी वह उसका समुचित निवेश कर सकता है जिससे उसे अतिरिक्त धन की प्राप्ति होती है । जो निवेश करने में जितना अधिक समर्थ होगा उसे उसी अनुपात में लाभ भी मिलेगा । जिसके पास धन ही न हो वह निवेश कहां से कर पाएगा ?
व्यवहारिक जीवन में उपर्युक्त बात कमोवेश सही ठहरती है बशर्ते कि हम धनसंपदा के अर्थ अधिक व्यापक लेते हुए उसमें बौद्धिक संपदा को भी जोड़ लें । आजकल बौद्धिक कौशल का जमाना है । आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए भी धनोपार्जन कर सकते हैं । ऐसा व्यक्ति पहले उसी का निवेश करता है, फिर उससे पाप्त धन का निवेश करता है । अंततः सभी को निवेश का ही रास्ता अपनाता होता है ।
मेरी समझ में चाणक्य का संदेश यही है कि भविष्यवाणी की ज्योतिष् या तत्सदृश कलाओं पर निर्भर न होकर व्यक्ति को अपने धन या हुनर से ही संपदा अर्जित करने की सोचनी चाहिए । – योगेन्द्र जोशी