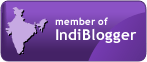इस चिट्ठे के छ: आलेखों की शृंखला की यह मेरी छ्ठी एवं अंतिम प्रविष्टि है। ध्यान रहे कि इन आलेखों में आदिशंकराचार्य द्वारा विरचित “चर्पटपञ्जरिकास्तोत्रम्” के १८ छंदों की चर्चा की जा रही है। (देखें इसका पूर्ववर्ती आलेख, दिनांक २३ मार्च, २०१७)
पहले आलेख में इस बात का उल्लेख किया गया था कि इस रचना में कुल सत्रह छंद हैं और उनके अतिरिक्त एक स्थायी छंद (भज गोविन्दं भज गोविन्दं …) भी है जो इनमें से प्रत्येक छंद के बाद प्रयुक्त हुआ है। यदि उक्त स्तोत्र को भजन के तौर पर गाया जाये तो यह छंद प्रत्येक के बाद गाया जायेगा। इसकी भूमिका गायन के स्थायी के समान है। इसे आगे उद्धृत किया जा रहा है:
[
भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते ।
प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुकृञ् करणे ॥
अर्थ – अरे ओ मूर्ख, गोविन्द का भजन कर यानी ईश्वर-भक्ति में मन लगा। जब तुम्हारा मरणकाल पास आ जायेगा तब यह “डुकृञ् करणे” की रट तुम्हें नहीं बचाएगी। “डुकृञ्” संस्कृत व्याकरण की एक क्रियाधातु है जिसका अर्थ “(कार्य/कर्तव्य) करना” है। इस क्रियाधातु का व्यवहार में प्रयोग सामान्यतः देखने को नहीं मिलता। अर्थात् इस पर बहुत दिमाग खपाना कुछ हद तक निरर्थक है। व्याकरण के अध्येता उक्त क्रियाधातु के अर्थ एवं प्रयोजन को याद रखने के लिए “डुकृञ् करणे” रटते होंगे जिसका तात्पर्य है “डुकृञ्” क्रिया “करण” (कार्य करना) के प्रयोजन में लिया जाता है । स्तोत्र के रचनाकार की दृष्टि में जीवन के अंतकाल तक सांसारिक कार्यों में ही निरंतर लिप्त रहना फलदायक नहीं है यह भाव “डुकृञ् करणे” के रटने में प्रतिबिंबित होता है। “अब तो इस रट को छोड़ो और ईश्वर-प्रार्थना में संलग्न होओ।”
]
चिट्ठे की मौजूदा प्रविष्टि में चर्पटपञ्जरिकास्तोत्रम् के अंतिम तीन छंद क्रमशः १५, १६, एवं १७ प्रस्तुत किये जा रहे हैं । इनमें पहला छंद है:
सुखतः क्रियते रामाभोगः पश्चाद्धन्त शरीरे रोगः ।
यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम् ॥१५॥ भज …
(रामा-भोगः सुखतः क्रियते, हन्त पश्चात् शरीरे रोगः, यद्यपि लोके मरणं शरणं, तत्-अपि पाप-आचरणम् न मुञ्चति।)
अर्थ – मनुष्य (पुरुष) स्त्री-संसर्ग का सुखभोग करता है, अफ़सोस कि बाद में शरीर रोगग्रस्त होता है। यद्यपि संसार में जीवन की अंतिम परिणति मृत्यु है, फिर भी मनुष्य पापकर्मों से अपने को मुक्त नहीं करता।
सांसारिक जीवन में स्त्री-पुरुष संबधों का सदा से महत्व रहा है और दोनों पक्ष (स्त्री एवं पुरुष) तत्संबंधित सुख पाने की लालसा करते हैं। मैं समझ नहीं पाया कि क्या श्रीशंकराचार्य दोनों के संसर्ग को रोग का कारण मानते हैं? या वे यह कहना चाहते हैं कि यौनसुख का समय भी उम्र के साथ समाप्त हो जाता है और रोगग्रस्तता का काल आ जाता है, क्योंकि रोगों का होना शरीर के अनेक दोषों में से एक है । हरएक को मृत्यु पूर्व भातिं-भांति की अवस्थाओं से गुजरना होता है। अस्तु, प्राणिमात्र को अंततः मृत्यु की शरण में ही जाना होता है। उसके बाद का उसका जीवन उसके पूर्व कर्मों पर निर्भर करता है। वे प्रश्न उठाते हैं कि इस तथ्य को जानने पर भी मनुष्य क्यों नहीं सत्कर्मों में लगता है?
एक बात जो मुझे विश्व में प्रचलित प्रायः सभी धर्मग्रंथों, नीति-पुस्तकों आदि में देखने को मिली है वह है कि उनमें प्रस्तुत प्रायः सभी बातें पुरुषों को केन्द्र में रखकर कही गई हैं। जैसे उपर्युक्त श्लोक में कहा गया कि पुरुष स्त्री-संसर्ग के सुख भोगता है। यह नहीं कहा गया है कि स्त्री पुरुष-संसर्ग का सुख भोगती है। धर्मग्रन्थों में – जितना मैं जान पाया – धर्मों की बातें प्रमुखतया पुरुषों के प्रति कही गयी हैं। सभी धर्म किसी पुरुष या किन्ही पुरुषों के वचनों पर आधारित रहे हैं। वस्तुतः स्त्रियों को शायद ही कहीं महत्व दिया गया है । सभी पैगंबर, तीर्थंकर, बौद्धधर्म-प्रवर्तक, वैदिक ऋषि, ईश्वरीय अवतार, आदि पुरुष ही रहे हैं। उक्त छंद में भी ऐसा ही है। सोचिए ऐसा क्यों है?
रथ्याकर्पटविरचितकन्थः पुण्यापुण्यविवर्जितपन्थः ।
नाहं न त्वं नायं लोकस्तदपि किमर्थं क्रियते शोकः ॥१६॥ भज …
(रथ्या-कर्पट-विरचित-कन्थः, पुण्य-अपुण्य-विवर्जित-पन्थः, न अहम् न त्वम् न अयम्, लोकः तत्-अपि किम्-अर्थंम् क्रियते शोकः)
अर्थ – रास्ते में पड़े चिथड़ों से बनी झोली या गुदड़ी काम चला लिया, पुण्य-अपुण्य से परे विशेष जीवन-मार्ग अपना लिया, न मैं हूं, न तुम हो, न ही यह संसार है यह जान लिया, तब भी किस बात शोक किया जाये।
उपर्युक्त कथन उस व्यक्ति के संदर्भ में संन्यास के मार्ग पर चल निकला हो। ऐसा व्यक्ति मार्ग में यानी आम जन से जो कुछ भी पा जाए उसी से काम चलाता है। चिथड़ों से बनी झोली या गुदड़ी से आशय इसी संसाधनविहीन जीवन को अविचलित भाव के साथ जीने से लिया जा सकता है।
पुण्यापुण्यविवर्जितपंथ” का अर्थ मेरी समझ में “पुण्यमय एवं अपुण्य से रहित मार्ग अपनाया हो जिसने” ऐसा होना चाहिए। अपेक्षा की जाती है कि संन्यासी पापमार्ग से बचा रहे। उसे जीवन की नश्वरता का ज्ञान जब हो जाता है तब उसे किसी प्रकार की हानि का भय नहीं रह जाता है।
कुरुते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनमथवा दानम्।
ज्ञानविहीनः सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्मशतेन ॥१७॥ भज …
(गङ्गा-सागर-गमनम्, व्रत-परि-पालनम्, अथवा दानम् कुरुते, ज्ञान-विहीनः सर्व-मतेन जन्म-शतेन मुक्तिम् न भजति ।)
अर्थ – गंगासागर पर तीर्थस्नान कर आवे, व्रत-उपवास करे अथवा दानादि सत्कर्म करे तो भी इन सभी साधनों/प्रयासों से ज्ञानहीन मनुष्य मुक्ति नहीं पाता है।
श्रीशंकराचार्य ज्ञानयोग के समर्थक थे। ज्ञान का तात्पर्य है अध्यात्मज्ञान। उनके अनुसार परमात्मा में विलीन होना यानी मोक्ष तभी मिलता है जब व्यक्ति को परामात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। उनके मतानुसार अन्य सभी पुण्यकर्म ज्ञानप्राप्ति में सहायक होते हैं, किंतु ज्ञान सर्वोपरि है। ज्ञान के अभाव में तीर्थ, व्रत, दान आदि के प्रयास स्वयं में फलदायक नहीं हो पाते हैं।
ये सब बातें उस जमाने की हैं जब संन्यास आश्रम जीवन के सभी बंधनों/आकर्षणों से मुक्ति के प्रयास की अवस्था हुआ करती थी। आज के युग में संन्यास जैसी चीज शायद ही कहीं हो। इस युग में संन्यास का अर्थ है गेरुआ वस्त्र धारण करके दूसरों की कमाई से सुखभोग प्राप्त करना। – योगेन्द्र जोशी