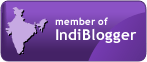करीब ढाई हजार वर्ष पूर्व भारतभूमि पर जिस मौर्य सामाज्य की स्थापना हुई थी उसका श्रेय उस काल के महान राजनीतिज्ञ चाणक्य को जाता है । राजनैतिक चातुर्य के धनी चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है । उनके बारे में मैंने पहले कभी अपने इसी ब्लॉग में लिखा है । कौटिलीय अर्थशास्त्र चाणक्य-विरचित ग्रंथ है, जिसमें राजा के कर्तव्यों का, आर्थिक तंत्र के विकास का, प्रभावी शासन एवं दण्ड व्यवस्था आदि का विवरण दिया गया है । उसी ग्रंथ के तीन चुने हुए श्लोकों का उल्लेख मैं यहां पर कर रहा हूं ।
(कौटिलीय अर्थशास्त्र, प्रथम अधिकरण, अध्याय 18)
1.
प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां तु हिते हितम् ।
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम् ॥
(प्रजा-सुखे सुखम् राज्ञः प्रजानाम् तु हिते हितम्, न आत्मप्रियम् हितम् राज्ञः प्रजानाम् तु प्रियम् हितम् ।)
प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है, प्रजा के हित में ही उसे अपना हित दिखना चाहिए । जो स्वयं को प्रिय लगे उसमें राजा का हित नहीं है, उसका हित तो प्रजा को जो प्रिय लगे उसमें है ।
2.
तस्मान्नित्योत्थितो राजा कुर्यादर्थानुशासनम्् ।
अर्थस्य मूलमुत्थानमनर्थस्य विपर्ययः ॥
(तस्मात् नित्य-उत्थितः राजा कुर्यात् अर्थ अनुशासनम्, अर्थस्य मूलम् उत्थानम् अनर्थस्य विपर्ययः ।)
इसलिए राजा को चाहिए कि वह नित्यप्रति उद्यमशील होकर अर्थोपार्जन तथा शासकीय व्यवहार संपन्न करे । उद्यमशीलता ही अर्थ (संपन्नता) का मूल है एवं उसके विपरीत उद्यमहीनता अर्थहीनता का कारण है ।
3.
अनुत्थाने ध्रुवो नाशः प्राप्तस्यानागतस्य च ।
प्राप्यते फलमुत्थानाल्लभते चार्थसम्पदम् ॥
(अनुत्थाने ध्रुवः नाशः प्राप्तस्य अनागतस्य च, प्राप्यते फलम् उत्थानात् लभते च अर्थ-सम्पदम् ।)
उद्यमशीलता के अभाव में पहले से जो प्राप्त है एवं भविष्य में जो प्राप्त हो पाता उन दोनों का ही नाश निश्चित है । उद्यम करने से ही वांछित फल प्राप्त होता है ओर उसी से आर्थिक संपन्नता मिलती है ।
कौटिल्य ने इन श्लोकों के माध्यम से अपना यह मत व्यक्त किया है कि राजा का कर्तव्य अपना हित साधना और सत्तासुख भोगना नहीं है । आज के युग में राजा अपवाद रूप में ही बचे हैं और उनका स्थान अधिकांश समाजों में जनप्रतिनिधियों ने ले लिया है जिन्हें आम जनता शासकीय व्यवस्था चलाने का दायित्व सोंपती है । कौटिल्य की बातें तो उन पर अधिक ही प्रासंगिक मानी जायेंगी क्योकि वे जनता के हित साधने के लिए जनप्रतिनिधि बनने की बात करते हैं । दुर्भाग्य से अपने समाज में उन उद्येश्यों की पूर्ति विरले जनप्रतिनिधि ही करते हैं ।
उद्योग शब्द से मतलब है निष्ठा के साथ उस कार्य में लग जाना जो व्यक्ति के लिए उसकी योग्यतानुसार शासन ने निर्धारित किया हो, या जिसे उसने अपने लिए स्वयं चुना हो । राजा यानी शासक का कर्तव्य है कि वह लोगों को अनुशासित रखे और कार्यसंस्कृति को प्रेरित करे । अनुशासन एवं कार्यसंस्कृति के अभाव में आर्थिक प्रगति संभव नहीं है । जिस समाज में लोग लापरवाह बने रहें, कार्य करने से बचते हों, समय का मूल्य न समझते हों, और शासन चलाने वाले अपने हित साधने में लगे रहें, वहां संपन्नता पाना संभव नहीं यह आचार्य कौटिल्य का संदेश है । – योगेन्द्र जोशी