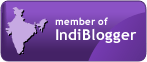29 सितम्बर 2014
by योगेन्द्र जोशी
in नीति, संस्कृत-साहित्य, हितोपदेश, Hitopadesh, Morals, Sanskrit Literature
टैग्स: ऊद्यमशील, दैव, नीतिवचन, भाग्य, हितोपदेश, destiny, Hitopadesh, Industrious, moral lesson
संस्कृत के नीतिविषयक ग्रंथों में से एक हितोपदेश है, जिसमें पशु-चरित्रों के माध्यम से आम जन के समक्ष महत्वपूर्ण सीख की बातें प्रस्तुत की गई हैं । उक्त ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय मैंने इसी ब्लॉग के 2 मार्च 2009 की पोस्ट में दिया है । यद्यपि यह ग्रंथ अवयस्कों-बालकों को संबोधित करके लिखा गया है, तथापि इसमें दी गई बातें सभी उम्र के लोगों के लिए उपयोगी हैं । ग्रंथ में एक स्थल पर “होनी टल नहीं सकती” यह कहते हुए भाग्य के भरोसे बैठ जाने की आलोचना की गई है । मैं तत्संबंधित दो श्लोकों का यहां पर उल्लेख कर रहा हूं:
यदभावि न तद्भावि भावि चेन्न तदन्यथा ।
इति चिन्ताविषघ्नो९यमगदः किं न पीयते ।।
(हितोपदेश, मित्रलाभ, 29)
(यत् अभावि न तत् भावि भावि चेत् न तत् अन्यथा इति चिन्ता-विषघ्नः अयम् अगदः किम् न पीयते ।)
अर्थ – “जो नहीं घटित होने वाला है वह होगा नहीं, यदि कुछ होने वाला हो तो वह टलेगा नहीं” इस विषरूपी चिंता (विचारणा) के शमन हेतु अमुक (आगे वर्णित) औषधि का सेवन क्यों नहीं किया जाता है ?
न दैवमपि सञ्चित्य त्यजेदुद्योगमात्मनः ।
अनुद्योगेन कस्तैलं तिलेभ्यः प्राप्तुमर्हति ।।
(यथा उपर्युक्त, 30)
(न दैवम् अपि सञ्चित्य त्यजेत् उद्योगम् आत्मनः न-उद्योगेन कः तैलं तिलेभ्यः प्राप्तुम् अर्हति ।)
अर्थ – (और औषधि यह है:) दैव यानी भाग्य का विचार करके व्यक्ति को कार्य-संपादन का अपना प्रयास त्याग नहीं देना चाहिए । भला समुचित प्रयास के बिना कौन तिलों से तेल प्राप्त कर सकता है ?
हितोपदेश के रचनाकार के मतानुसार पुरुषार्थ यानी उद्यम के बिना वांछित फल नहीं मिल सकता है । “जो होना (या नहीं होना) तय है वह तो होगा ही (या होगा ही नहीं)” यह विचार मान्य नहीं हो सकता । यह सही है कि जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता है । अर्थात् जो घटना भूतकाल का हिस्सा हो चुकी हो उसे कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है । यह भी संभव है कि जो भविष्य में होना हो वह भी हो के रहे । परंतु यह कौन बताएगा कि वह भावी घटना क्या होगी ? जब वह घटित हो जाए तब तो वह भूतकाल का अंग बन जाता है और उसके बारे में “यह तो होना था” जैसा वक्तव्य दिया जा सकता है । लेकिन जब तक वह घटित न हो जाए तब तक कैसे पता चलेगा कि क्या होने वाला है ? ऐसी स्थिति में क्या यह नहीं स्वीकारा जाना चाहिए कि उस भावी एवं अज्ञात घटना को संपन्न करने हेतु किए जाने वाले हमारे प्रयास उसके घटित होने के कारण होते हैं । अवश्य ही कुछ ऐसे कारक भी घटना को प्रभावित करते होंगे जिन पर हमारा नियंत्रण न हो अथवा वे पूर्णतः अज्ञात हों । उन कारकों एवं हमारे प्रयासों के सम्मिलित प्रभाव के अधीन ही वह घटना जन्म लेगी जिसके घटित हो चुकने पर ही वह अपरिवर्तनीय कही जाएगी । किंतु उस क्षण से पहले हम जान नहीं सकते कि वह घटना क्या होगी । अतः हमारे प्रयास चलते रहने चाहिए । – योगेन्द्र जोशी
28 जुलाई 2014
by योगेन्द्र जोशी
in धर्म, नीति, महाभारत, राजनीति, शासन, संस्कृत-साहित्य, Government, Mahabharata, Morals, Politics, religion, Sanskrit Literature, Uncategorized
टैग्स: भीष्म उपदेश, महाभारत, शासक के कर्तव्य, शासक के लिए दंड, स्त्री सम्मान, Duties of Ruler, Mahabharata, Punishment to Ruler, Respecting Women, Teachings of Bhishma
भारतीयों के लिए वेदव्यासरचित महाकाव्य महाभारत एक सुपरिचित ग्रंथ है जिसकी कथाओं का जिक्र लोग यदाकदा करते रहते हैं । महाभारत में वर्णित पांडव-कौरवों के युद्ध की समाप्ति के बाद राजा युधिष्ठिर सरशय्या पर लेटे भीष्म पितामह से राजकार्य संबंधी नीतिवचन प्राप्त करते हैं । राजा के लिए क्या कृत्य है क्या नहीं इस बाबत अनेकानेक बातें भीष्म बताते हैं । उसी प्रकरण में वे यह भी कहते हैं कि उस राजा को प्रजा ने मृत्युदंड दे देना चाहिए जो उनकी सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेता है । मैं तत्संबंधित तीन श्लोकों की चर्चा यहां पर कर रहा हूं । ये तीनों महाभारत के अनुशासनपर्व (अध्याय ६१) से उद्धृत किए जा रहे हैं ।
क्रोश्यन्त्यो यस्य वै राष्ट्राद्ध्रियन्ते तरसा स्त्रियः ।
क्रोशतां पतिपुत्राणां मृतोऽसौ न च जीवति ॥३१॥
(महाभारत, अनुशासनपर्व, अध्याय ६१)
(यस्य वै राष्ट्रात् क्रोशताम् पतिपुत्राणाम् क्रोश्यन्त्यः स्त्रियः तरसा ध्रियन्ते असौ मृतः न च जीवति ।)
अर्थ – जिस राजा के राज्य में चीखती-चिल्लाती स्त्रियों का बलपूर्वक अपहरण होता है और उनके पति-पुत्र रोते-चिल्लाते रहते हैं, वह राजा मरा हुआ है न कि जीवित ।
जो राजा अपहरण की जा रही स्त्रियों की सुरक्षा के लिए समुचित कदम नहीं उठाता और उनके दुःखित बंधु-बांधवों की विवशता से विचलित नहीं होता वह जीते-जी मरे हुए के समान है । उसके जीवित होने की कोई सार्थकता नहीं रह जाती ।
ध्यान रहे कि आज के लोकतांत्रिक शासकीय व्यवस्था में जो सत्ता के शीर्ष पर हो वही राजा की भूमिका निभाता है । इसलिए राजा के संदर्भ में जो बातें कही गई हैं वह आज के शासकों पर यथावत लागू होती हैं । अपने देश के कुछ राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश, में इस समय स्त्रियों के प्रति दुष्कर्म के मामले चरम पर हैं, किंतु शासकीय व्यवस्था इतनी गिरी हुई है कि किसी को दंडित नहीं किया जा रहा है । ऐसे शासकों को वस्तुतः डूब मरना चाहिए!
अरक्षितारं हर्तारं विलोप्तारमनायकम् ।
तं वै राजकलिं हन्युः प्रजाः सन्नहा निर्घृणम् ॥३२॥
(यथा पूर्वोक्त)
(अरक्षितारम् हर्तारम् विलोप्तारम् अनायकम् तम् निर्घृणम् राजकलिम् प्रजाः वै सन्नहा हन्युः ।)
अर्थ – जो राजा अपनी जनता की रक्षा नहीं करता, उनकी धनसंपदा छीनता या जब्त करता है, जो योग्य नेतृत्व से वंचित हो, उस निकृष्ट राजा को प्रजा ने बंधक बनाकर निर्दयतापूर्वक मार डालना चाहिए ।
राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना, उसको सुख-समृद्धि के अवसर प्रदान करना । तभी वह जनता से कर वसूलने का हकदार बन सकता है । अपने कर्तव्यों का निर्वाह न करने वाला राजा जब कर वसूले तो उसको लुटेरा ही कहा जाएगा । नीति कहती है कि ऐसे राजा को निकृष्ट कोटि का मानना चाहिए । उसके प्रति दयाभाव रखे बिना ही परलोक भेज देना चाहिए ।
आज की शासकीय स्थिति कुछ राज्यों में अति दयनीय है । परंतु दुर्भाग्य से सत्तासुख भोग रहे वहां के शासकों को दंडित करने वाला कोई नहीं । लोग कहते हैं कि पांच-पांच सालों में होने वाले चुनावों द्वारा जनता उन्हें सत्ता से बेदखल कर देती है । लेकिन ध्यान दें कि न चुना जाना कोई दंड नहीं होता है । किसी भी चुनाव में कई प्रत्याशी भाग लेते हैं जिनमें से एक चुना जाता है । “अन्य सभी को दंडित कर दिया” ऐसा क्या कहा जा सकता है ? सवाल असल में दंडित किये जाने का है जो वास्तव में होता नहीं ।
अहं वो रक्षितेत्युक्त्वा यो न रक्षति भूमिपः ।
स संहत्य निहंतव्यः श्वेव सोन्मादः आतुरः ॥३३॥
(यथा पूर्वोक्त)
(अहम् वः रक्षिता इति उक्त्वा यः भूमिपः न रक्षति सः स-उन्मादः आतुरः श्व-इव संहत्य निहंतव्यः ।)
अर्थ – मैं आप सबका रक्षक हूं यह वचन देकर जो राजा रक्षा नहीं करता, उसे रोग एवं पागलपन से ग्रस्त कुत्ते की भांति सबने मिलकर मार डालना चाहिए ।
इस श्लोक में कटु शब्दों का प्रयोग हुआ है । शासक का पहला कर्तव्य है कि वह भयमुक्त समाज की रचना करे – भयमुक्त निरीह-निरपराध प्रजा के लिए, न कि अपराधियों के लिए । आज की स्थिति उल्टी है । अपराधी निरंकुश-स्वच्छंद विचरण करते हुए और सामान्य जन डरे-सहमे दिखते हैं । जिस शासक के राज्य में ऐसा हो उसे ग्रंथकार ने पागल कुत्ते की संज्ञा दी है । ऐसे कुत्ते का एक ही इलाज होता है, मौत । दुर्भाग्य से हमारे शासक सबसे पहले अपनी सुरक्षा का इंतजाम करते हैं । कोई सामान्य व्यक्ति उनके पास पहुंच तक नहीं सकता, आगे कुछ करने का तो सवाल ही नहीं ।
ये नीतिश्लोक दर्शाते हैं कि महाभारत ग्रंथ में कर्तव्यों में विफल शासक को पतित और निकृष्ट श्रेणी का कहा गया है । – योगेन्द्र जोशी
13 दिसम्बर 2013
by योगेन्द्र जोशी
in चाणक्य नीति, नीति, राजनीति, सूक्ति, Chanakya Niti, Morals, Politics
टैग्स: कौटिलीय अर्थशास्त्र, कौटिल्य, चाणक्य, दंडित करने की नीति, भ्रष्ट अधिकारी, Chanakya, Corrupt Officers, Kautiliya Arthashastra, Kautilya, Policy of Punishment
इस ब्लॉग की पिछली पोस्ट में मैंने चाणक्य-विरचित “कौटिलीय अर्थशास्त्र” की चर्चा की थी । तब मैंने उस ग्रंथ में उल्लिखित भ्रष्टाचार तथा भ्रष्ट अधिकारियों से संबंधित 5 श्लोकों में से 3 को उद्धृत किया था । शेष 2 श्लोकों को मैं यहां लिख रहा हूं:
आस्रावयेच्चोपचितान् विपर्यस्येच्च कर्मसु ।
यथा न भक्षयन्त्यर्थं भक्षितं निर्वमन्ति वा ॥
(उपचितान् च आस्रावयेत् विपर्यस्येत् च कर्मसु, यथा अर्थम् न भक्षयन्ति भक्षितम् वा निर्वमन्ति ।)
(कौटिलीय अर्थशास्त्र, द्वितीय अधिकरण, प्रकरण 25)
अर्थ – सरकारी धन संबंधी दायित्व में लगाए व्यक्तियों से पैसा (दंडस्वरूप) वसूला जाना चाहिए और उनकी पदावनति की जानी चाहिए, ताकि वे फिर धन का भक्षण न कर सकें और जो भक्षण किया हो उसको उगल दें ।
शासन द्वारा नियुक्त अधिकारी धन का दुरुपयोग मूलतः दो प्रकार से करते हैं । एक तो यह है कि वह किसी कार्यविशेष के लिए आबंटित धन को पूरा या अंशतः, अकेले या अन्य जनों से मिलकर, हड़प जाए; दूसरा यह कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों एवं कार्य से संबंधित अन्य व्यक्तियों की उचित निगरानी नहीं करता, जिससे वे धनका लाभ स्वयं उठाते हैं और दूसरों को उठाने देते हैं । कौटिल्य (चाणक्य) के अनुसार पहली स्थिति में उस अधिकारी से दायित्व छीन लेना चाहिए, साथ ही उसकी पदावनति की जानी चाहिए अथवा उसे पदमुक्त कर देना चाहिए । इसी के साथ उसके द्वारा अर्जित धन छीन लेना चाहिए । दूसरी स्थिति में कार्यमुक्त करते हुए उसकी पदावनति की जानी चाहिए । उदाहरणार्थ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर नजर न रखने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए, भले ही वह उस कार्य में धन न कमा रहा हो । कार्य के प्रति लापरवाही भी दंडनीय है ।
न भक्षयन्ति ये अर्थान् न्यायतो वर्धयन्ति च ।
नित्याधिकाराः कार्यास्ते राज्ञः प्रियहिते रताः ॥
(ये अर्थान् न भक्षयन्ति न्यायतः वर्धयन्ति च, राज्ञः प्रिय-हिते रताः ते नित्य-अधिकाराः कार्याः ।)
(कौटिलीय अर्थशास्त्र, द्वितीय अधिकरण, प्रकरण 25)
अर्थ – जो कर्मचारी राजा का धन नहीं हड़पते, बल्कि उसे न्यायसम्मत तरीके से बढ़ाते हैं, राजा के प्रियदायक हितों में संलग्न रहने वाले वैसे कर्मियों को अधिकारियों के तौर पर कार्य में नियुक्त किया जाना चाहिए ।
पूर्वकाल में राजकीय व्यवस्था प्रायः सभी समाजों में प्रचलित थी तदनुसार राजकीय कोष को राजा का धन कहा जाता है । उसी धन से सभी विकास एवं जनसुविधाओं के कार्य किए जाते थे । आज के संदर्भ में राजा उस संस्था को व्यक्त करता है जो देश की शासकीय व्यवस्था चलाती है । विभिन्न स्रोतों से धन एकत्रित करना और उसे जनकल्याण आदि के कायों में लगाना उसी संस्था का दायित्व होता है । धन प्राप्ति, उसका संचय तथा समुचित व्यय प्रशासनिक तंत्र द्वारा राजाओं के काल में और आज के लोकतंत्रों या अन्य शासकीय व्यवस्थाओं में किया जाता है । उक्त नीतिवचन इस मत पर जोर डालता है कि धन संबंधी तमाम कार्यों में संलग्न अधिकारियों पर राजा या शासकों की पैनी दृष्टि रहनी चाहिए कि वे निष्ठा से कार्य कर रहे कि नहीं । जो व्यक्ति राजकोश को हानि पहुंचा रहा हो उसे तुरंत जिम्मेदारी के पद से हटाया जाना चाहिए, उसके पदावनत कर देना चाहिए और उससे कोश को पहुंचे नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए ।
दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसे लोगों के विरुद्ध सामान्यतः कोई कार्रवाई नहीं होती है । चूंकि सरकारी मुलाजिमों को उचित दंड नहीं दिया जाता है, अतः भ्रष्टाचार करने से कोई डरता नहीं । – योगेन्द्र जोशी
(यहां प्रस्तुत जानकारी चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, द्वारा प्रकाशित कौटिलीय अर्थशास्त्र, संस्करण 2006, पर आधारित है ।)
27 नवम्बर 2013
by योगेन्द्र जोशी
in धर्म, नीति, राजनीति, संस्कृत-साहित्य, सूक्ति, Morals, Politics, religion, Sanskrit Literature
टैग्स: आर्थिक भ्रष्टाचार, कौटिलीय अर्थशास्त्र, कौटिल्य, चाणक्य, सरकारी कर्मचारी, Chanakya, Financial Corruption, Government Official., Kautileeya Arthashastra, Kautilya
आचार्य चाणक्य के नाम से प्रायः सभी परचित होंगे । चणक के पुत्र होने के कारण उनको चाणक्य कहा जाता था, अन्यथा उनका नाम विष्णुदत्त था । उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है । मैंने पहले कभी लिखी गई एक पोस्ट में उनका संक्षिप्त परिचय दिया है ।
“कौटिलीय अर्थशास्त्र” चाणक्यरचित एक ग्रंथ है, जिसमें राजा, राजकर्मचारियों एवं प्रजा के अलग-अलग क्षेत्रों में भूमिकाओं तथा कर्तव्यों का विवरण दिया गया है । उसके एक अध्याय में भ्रष्टाचार तथा भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में लिखा गया है । मैं यहां पर तत्संबंधित 5 श्लोकों में से 3 को उद्धृत कर रहा हूं ।
यथा ह्यनास्वादयितुं न शक्यं जिह्वातलस्थं मधु वा विषं वा ।
अर्थस्तथा ह्यर्थचरेण राज्ञः स्वल्पोऽप्यनास्वादयितुं न शक्यः ॥
(यथा हि जिह्वा-तलस्थम् मधु वा विषम् वा न-आस्वादयितुम् न शक्यम्, तथा हि राज्ञः अर्थचरेण अर्थः स्वल्पः अपि न-आस्वादयितुं न शक्यः ।)
(यह तथा आगे दिए गए नीतिवचन कौटिलीय अर्थशास्त्र, द्वितीय अधिकरण, प्रकरण 25 से लिए गए हैं ।)
अर्थ – जिस प्रकार जीभ पर रखे शहद अथवा विष का रसास्वादन किए बिना नहीं रहा जा सकता है, ठीक वैसे ही राजा द्वारा आर्थिक प्रबंधन में लगाए गए व्यक्ति द्वारा धन का थोड़ा भी स्वाद न लिया जा रहा हो यह संभव नहीं ।
तात्पर्य यह है कि जो चीज आपके मुख में आ चुकी है उसका स्वाद कैसा है यह तो आपको पता चलेगा ही । और यदि वह स्वाद मन माफिक हुआ तो उसका आकर्षण तो अनुभव करेंगे ही, अधिक नहीं तो कुछ तो उसे और चखने की लालसा आपमें जग सकती है । कौटिल्य के अनुसार कुछ ऐसा ही राजकीय धन के साथ भी हो सकता है । जिस व्यक्ति को उसे संचित रखने या सही तरीके से खर्चने की जिम्मेदारी दी गई हो उसके मन में उसका कुछ हिस्सा पाने का, उससे कुछ लाभ कमाने का, लालच कदाचित उपज सकता है । उसमें से कुछ चुंगी अपने नाम करने में वह संभवतः हिचके ही नहीं । यह चुंगी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष तौर पर लिया जा सकता है, जैसे दलाली के रूप में । बिरले ही होते हैं जो इस लालच से अपने को मुक्त रखना चाहते हों या रख पाते हों ।
मत्स्या यथान्तःसलिले चरन्तो ज्ञातं न शक्याः सलिलं पिबन्तः ।
युक्तास्तथा कार्यविधौ नियुक्ता ज्ञातुं न शक्या धनमाददानाः ॥
(मत्स्याः यथा अन्तः-सलिले चरन्तः सलिलम् पिबन्तः ज्ञातुम् न शक्याः, तथा कार्य-विधौ युक्ताः नियुक्ताः धनम् आददानाः ज्ञातुम् न शक्याः ।)
अर्थ – जैसे पानी के अंदर चलायमान मछलियों का पानी पीना जाना नहीं जा सकता, वैसे ही कार्य-संपादन में लगाये जाने पर नियुक्त अधिकारियों द्वारा धन के अपहरण को नहीं जाना जा सकता है ।
राजस्व एकत्रित करने अथवा उसे उचित प्रकार से खर्चने की जिन अधिकारियों पर जिम्मेदारी होती है वे वस्तुतः कितनी ईमानदारी बरत रहे हैं यह आम जन प्रत्यक्षतः नहीं जान पाते हैं, क्योंकि उनके पास संबंधित धनराशि और उसके उपयोग का विवरण नहीं होता । जब कोई संस्था या व्यक्ति काफी मेहनत और छानबीन से जानकारी इकठ्ठा करता है तभी लोग कुछ जान पाते हैं । इसीलिए यह कहा जा सकता है कि पता नहीं वे क्या और कैसे कार्य कर रहे हैं ।
अपि शक्या गतिर्ज्ञातुं पततां खे पतत्त्रिणाम् ।
न तु प्रच्छन्नभावानां युक्तानां चरतां गतिः ॥
(खे पतताम् पतत्त्रिणाम् गतिः ज्ञातुम् अपि शक्या, न तु चरताम् प्रच्छन्न-भावानाम् युक्तानाम् गतिः ।)
अर्थ – आसमान में उड़ रहे पक्षियों की गति का ज्ञान पाना संभव है, किंतु कार्य में लगाए गए छिपे हुए भावों वाले व्यक्तियों के दायित्व-निर्वाह-प्रणाली को समझ पाना संभव नहीं ।
कहने का मतलब यह है कि उड़ते पक्षी किधर एवं किस रफ्तार से उड़ रहे है इसे उन पर नजर डालकर सामान्य व्यक्ति काफी हद तक समझ सकता है । उनका व्यवहार संदिग्ध नहीं होता । सरकारी कर्मचारी क्या सोच के बैठा है, वह दिखा क्या रहा है और वास्तव में क्या करने का इरादा रखता है, यह सब सरलता से नहीं जाना जा सकता है ये बातें । अपने देश में आजकल के घटित हो रहे आर्थिक अपराधों से समझ में आ जाती हैं । जब सब कुछ घट जाता है तब समझ में आता है कि बहुत कुछ गलत हो रहा है । तब भी यह स्पष्ट हो पाता है कि वास्तव में कौन जिम्मेदार है । यही कारण है कि देश में अपराधों की बाढ़ तो आ रही लेकिन दंडित बिरले ही होते हैं ।
लोभ-लालच-लालसा मनुष्य में तमाम अन्य गुणावगुणों की भांति स्वभावतः विद्यमान रहते हैं । इनकी मौजूदगी कभी धन-लोलुपता के रूप में स्वयं को उजागर करती है, तो कभी समाज में प्रतिष्ठित पदों पर पहुंचने अथवा कभी लोगों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के तौर पर, इत्यादि । इनको प्राप्त करने के लिए अनुचित कदम भी उठाने की इच्छा यदाकदा मनुष्य में जागने लगती है । किंतु सभ्य मानव समाज के मूल्य मनुष्य को आत्मसंयमित रहने को प्रेरित करते हैं । फिर भी सभी मनुष्य चारित्रिक तौर पर पर्याप्त सक्षम नहीं होते और इसी कारण अपनी लालसाओं को पूरा करने वे को भ्रष्टाचार का मार्ग अपना लेते हैं । कौटिलीय अर्थशास्त्र के उपर्युक्त वचन यह स्पष्ट करते हैं कि भ्रष्टाचार समाज में सदा से रहा है । हां, ढाई हजार वर्ष पूर्व की तुलना में आज यह अधिक व्यापकता पा चुका है । वस्तुतः इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि ही हो रही है । – योगेन्द्र जोशी
(यहां प्रस्तुत जानकारी चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, द्वारा प्रकाशित कौटिलीय अर्थशास्त्र, संस्करण 2006, पर आधारित है ।)
अंत में भोजपुर मंदिर (भोपाल के पास) की तस्वीर –

13 अगस्त 2013
by योगेन्द्र जोशी
in धर्म, नीति, महाभारत, संस्कृत-साहित्य, सूक्ति, Mahabharata, Morals, religion, Sanskrit Literature
टैग्स: abusive words, अपशब्द, कटु वचन, नीति, ययाति एवं पुरु, सामाजिक प्रतिष्ठा, harsh words, morals, social dignity, Yayati and Puru
महाकाव्य महाभारत के एक प्रकरण का उल्लेख करते हुए मैंने विगत दो ब्लॉग प्रविष्टियों, क्रमशः दिनांक ९ जुलाई एवं ५ अगस्त, तथा में महाराज ययाति का अपने ज्येष्ठ पुत्र पुरु को दिए गए उपदेशों की चर्चा की थी । उन्हीं उपदेशों की शृंखला के तीन अतिरिक्त श्लोक मैं यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं:
वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति यैराहतः शोचन्ति रात्र्यहानि ।
परस्य नामर्मसु ते पतन्ति तान् पण्डितो नावसृजेत परेषु ॥
(महाभारत, आदिपर्व, अध्याय , श्लोक 11)
(वदनात् वाक्-सायकाः निष्पतन्ति यैः आहतः रात्रि-अहानि शोचन्ति, ते परस्य अमर्मसु न पतन्ति, पण्डितः तान् परेषु न अवसृजेत ।)
अर्थ – कठोर वचन रूपी बाण (दुर्जन) लोगों के मुख से निकलते ही हैं, और उनसे आहत होकर अन्य जन रातदिन शोक एवं चिंता के घिर जाते हैं । स्मरण रहे कि ये वाग्वाण दूसरे के अमर्म यानी संवेदनाशून्य अंग पर नहीं गिरते, अतः समझदार व्यक्ति ऐसे वचन दूसरों के प्रति न बोले ।
दूसरे के अमर्म पर नहीं गिरते कहना आलंकारिक कथन है; तात्पर्य है कि मर्म अथवा हृदय पर ही वे आघात करते न कि अन्यत्र । दूसरों के कटु वचन किसी को कितना आहत करेंगे यह उस व्यक्ति की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है । बहुत से लोग सब कुछ पचा जाते हैं । लेकिन संसार में भावुक प्रकृति के ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरे के कटु वचन से परेशान हो जाते हैं और अपनी रातों की नींद भी खो बैठते हैं । ऐसे ही लोगों के प्रति सतर्क रहने की सलाह इस श्लोक में दी गई है ।
न हीदृशं संवननं त्रिषु लोकेषु वर्तते ।
दया मैत्री च भूतेषु दानं च मधुरा च वाक ॥
(पूर्वोक्त, श्लोक 12)
(त्रिषु लोकेषु ईदृशं संवननम् न हि वर्तते, भूतेषु दया मैत्री च दानम् च मधुरा च वाक ।)
अर्थ – प्राणियों के प्रति दया, सौहार्द्र, दानकर्म, एवं मधुर वाणी के व्यवहार के जैसा कोई वशीकरण का साधन तीनों लोकों में नहीं है ।
मेरी समझ में इस स्थल पर वशीकरण का तात्पर्य कदाचित् दूसरे को अपने पक्ष में करना है किसी प्रकार के दबाव बिना, महज अपने सद्व्यवहार से । ऐसा बरताव दूसरे के प्रति करना चाहिए कि वे स्वयं ही आपके प्रति सम्मानभाव रखने लगें । तीन लोक होते हैं अथवा नहीं इसका भी महत्व नहीं है । संकेत इस बात के प्रति है कि सर्वत्र ही व्यक्ति का व्यवहार दूसरों को प्रभावित करता है ।
आज के युग में ये बातें किस हद तक मान्य हो सकती हैं इस पर मुझे शंका है । मुझे तो यह अनुभव होने लगा है कि समाज में अयोग्य व्यक्ति पूजे जा रहे है और योग्य व्यक्ति तिरस्कृत हो रहे हैं । कदाचारियों की संख्या दिनबदिन बढ़ रही है ।
तस्मात्सान्त्वं सदा वाच्यं न वाच्यं परुषं क्वचित् ।
पूज्यान् सम्पूजयेद्दद्यान्न च याचेत् कदाचन ॥
(पूर्वोक्त, श्लोक 13)
(तस्मात् सदा सान्त्वम् वाच्यं परुषम् न क्वचित् वाच्यम्, पूज्यान् सम्पूजयेद् दद्यात् कदाचन न च याचेत् ।)
अर्थ – अतः सदा ही दूसरों से सान्त्वनाप्रद शब्द बोले, कभी भी कठोर वचन न कहे । पूजनीय व्यक्तियों के सम्मान व्यक्त करे । दूसरों यथासंभव दे और स्वयं किसी से मांगे नहीं ।
ये पुरु को संबोधित ययाति के उपदेशों के अंतिम शब्द हैं, जिनमें सबके प्रति सद्व्यवहार की, अपनी तुलना में पूज्य जनों का समादर करने की, दूसरों को दान देने की, और उनसे कुछ पाने की लालसा न रखने की सलाह अभिव्यक्त है । – योगेन्द्र जोशी
05 अगस्त 2013
by योगेन्द्र जोशी
in धर्म, नीति, महाभारत, संस्कृत-साहित्य, सूक्ति, Mahabharata, Morals, Sanskrit Literature
टैग्स: anger, क्रोध, नीति, ययाति एवं पुरु, सहिष्णुता, सामाजिक प्रतिष्ठा, morals, social dignity, tolerance, Yayati and Puru
महाकाव्य महाभारत के एक प्रकरण का उल्लेख करते हुए मैंने पिछली पोस्ट में महाराज ययाति का अपने ज्येष्ठ पुत्र पुरु को दिए गए उपदेशों की चर्चा की थी । उन्हीं उपदेशों की शृंखला के तीन अन्य श्लोक मैं यहां पर उद्धृत कर रहा हूं:
नारुन्तुदः स्यान्न नृशंसवादी न हीनतः परमभ्याददीत ।
ययास्य वाचा पर उद्विजेत न तां वदेदुषतीं पापलोक्याम् ॥
(महाभारत, आदिपर्व, अध्याय , श्लोक ८)
(न अरुन्तुदः स्यात् न नृशंस-वादी न हीनतः परम् अभि-आददीत, अस्य यया वाचा परः उद्विजेत ताम् उषतीम् पाप-लोक्याम् न वदेत् ।)
अर्थ – दूसरे के मर्म को चोट न पहुंचाए, चुभने वाली बातें न बोले, घटिया तरीके से दूसरे को वश में न करे, दूसरे को उद्विग्न करने एवं ताप पहुंचाने वाली, पापी जनों के आचरण वाली बोली न बोले ।
शरीर के अतिसंवेदनशील अंग को मर्म कहा जाता है । यह वह स्थल होता है जहां हल्की चोट का लगना भी अत्यंत कष्टदायक एवं असह्य होता है । मर्म शब्द हृदय अथवा मन के लिए भी प्रयुक्त होता है । मनुष्य को दो प्रकार से चोट पहुंचाई जा सकती है; पहला है कि शरीर के अंगविशेष पर प्रहार करना, और दूसरा है कटु वचनों के द्वारा मन को आघात पहुंचाना । आम तौर पर लोग अप्रिय वचनों से ही दूसरों को आहत करते हैं । उक्त नीतिवचन में कदाचित् ऐसा न करने की सलाह है । यह भी कहा है कि दूसरे को घटिया तरीके से अपने वश में न करे । दूसरों को नियंत्रण में लेने हेतु बलप्रयोग करके जंजीर से बांधकर रखना, कोठरी में बंद करना, परिवार के सदस्य का अपहरण करके या वैसी धमकी देकर किसी को अपने अधीन रखना, आदि ऐसे क्रूर तरीके हैं जिनसे बचने की सलाह उक्त श्लोक में निहित है ।
अरुन्तुदं परुषं तीष्णवाचं वाक्कण्टकैर्वितुदन्तं मनुष्यान् ।
विद्यादलक्ष्मीकतमं जनानां मुखे निबद्धां निर्ऋतिं वहन्तम् ॥
(पूर्वोक्त, श्लोक ९)
(अरुन्तुदम् परुषम् तीष्ण-वाचम् वाक्-कण्टकैः मनुष्यान् वितुदन्तम्, मुखे निबद्धाम् निर्ऋतिम् वहन्तम् जनानाम् अलक्ष्मीक-तमम् विद्यात् ।)
अर्थ – मर्म को चोट पहुंचाने वाली, कठोर, तीखी, कांटों के समान लोगों को चुभने वाली बोली बोलने वाले व्यक्ति को लोगों के बीच विद्यमान सर्वाधिक श्रीविहीन और मुख में पिशाचिनी का वहन करने वाले मनुष्य के तौर पर देखा जाना चाहिए ।
दूसरों के साथ कटु व्यवहार करने वाले को श्रीविहीन कहा गया है । व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर ही समाज में किसी की प्रतिष्ठा अथवा निंदा होती है । धनवान या राजनैतिक बल आदि से लोगों के बीच झूठी और अस्थाई शान संभव है, किंतु उसे श्रीहीन ही समझा जाएगा इस श्लोक का यही आशय है ।
सद्भिः पुरस्तादभिपूजितः स्यात् सद्भिस्तथा पृष्ठतो रक्षितः स्यात् ।
सदासतामतिवादांस्तितिक्षेत् सतां वृत्तं चाददीतार्यवृत्तः ॥
(पूर्वोक्त, श्लोक १०)
(सद्भिः पुरस्तात् अभिपूजितः स्यात् तथा सद्भिः पृष्ठतः रक्षितः स्यात्, असताम् अतिवादान् सदा तितिक्षेत् आर्यवृत्तः सताम् वृत्तम् च आददीत ।)
अर्थ – व्यक्ति के कर्म ऐसे हों कि सज्जन लोग उसके समक्ष सम्मान व्यक्त करें ही, परोक्ष में भी उनकी धारणाएं सुरक्षित रहें । दुष्ट प्रकृति के लोगों की ऊलजलूल बातें सह ले, और सदैव श्रेष्ठ लोगों के सदाचारण में स्वयं संलग्न रहे ।
आम लोगों के आचरण में यह देखा जाता है कि वे सामने पड़ने पर तो चिकनी-चुपड़ी बातों से सम्मान प्रदर्शित करते हैं, लेकिन पीठ पीछे बुरा-भला भी कहने से नहीं बचते । ऐसे लोगों के कथनों से सदाचारी व्यक्ति को विचलित नहीं होना चाहिए । उसका यत्न होना चाहिए कि लोग उसकी अनुपस्थिति में भी उसके बारे में सम्मानजनक बातें करें, और वह हर दशा में अपने सदाचरण पर टिका रहे । वास्तव में दूसरों के उल्टेसीधे बोल उनके अपने ही व्यक्तित्व के दोष होते हैं । – योगेन्द्र जोशी
09 जुलाई 2013
by योगेन्द्र जोशी
in धर्म, नीति, महाभारत, लोकव्यवहार, सूक्ति, Mahabharata, Morals, religion
टैग्स: anger, क्रोध, नीति, ययाति एवं पुरु, सहिष्णुता, morals, Yayati and Puru
महाकाव्य महाभारत में एक प्रकरण का वर्णन है जिसमें महाराज ययाति अपने ज्येष्ठ पुत्र पुरु को मानवीय गुणों को अपनाने का उपदेश देते हैं । पिता-पुत्र के बारे में कथा है कि ययाति जब वृद्ध हो चले परंतु ऐहिक भोग-विलास से उनकी तृप्ति नहीं हो सकी थी तो युवराज पुरु ने अपना यौवन उन्हें प्रदान कर दिया और स्वयं उनका वार्धक्य ग्रहण कर लिया । मैं इस कथा के विस्तार में नहीं जा रहा हूं । महाभारत के अनुसार कौरव-पांडव ययाति-पुत्र पुरु के अनेकों पिढ़ियों बाद के वंशज थे । उसी वंशशृंखला में दुश्यंत, भरत एवं शांतनु चर्चित राजा हुए थे । मैं जिन उपदेशों की चर्चा कर रहा हूं वे आठ श्लोकों में निबद्ध हैं, जिनमें से प्रथम दो का उल्लेख में इस स्थल पर कर रहा हूं:
अक्रोधनो क्रोधनेभ्यो विशिष्टस्तथा तितिक्षुरतितिक्षोर्विशिष्टः ।
अमानुषेभ्यो मानुषाश्च प्रधाना विद्वांस्तथैवाविदुषः प्रधानः ॥
(महाभारत, आदिपर्व, अध्याय , श्लोक 6)
(अक्रोधनः क्रोधनेभ्यः विशिष्टः तथा तितिक्षुः अतितिक्षोः विशिष्टः, अमानुषेभ्यः च मानुषाः प्रधानाः तथा एव विद्वान् अविदुषः प्रधानः ।)
अर्थ – क्रोध न करने वाला क्रोधी व्यक्ति से और सहनशील व्यक्ति असहिष्णु से विशेषतर यानी श्रेष्ठतर होता है; इसी प्रकार अमनुष्य मनुष्यों एवं विद्वान अविद्वान की तुलना में श्रेष्ठतर होते हैं ।
क्रोध तथा असहिष्णुता उच्च जीवधारियों (पशुओं) की स्वाभाविक वृत्तियां हैं, जिन्हें अर्जित करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है । प्रयास तो इन पर नियंत्रण पाने की क्षमता पाने के लिए करना पड़ता है; जिसने नियंत्रण पा लिया हो, वह समाज में निःसंदेह विशेष स्थान का हकदार कहलाएगा । इसी प्रकार विद्वान होना भी व्यक्ति की प्रशंसनीय उपलब्धि है । ‘अमानुष’ का शाब्दिक अर्थ मनुष्य से इतर ‘प्राणी’ होता है, किंतु यहां पर इसे उस पुरुष के लिए प्रयोग में लिया गया है जिसमें अपेक्षित मानवीय गुणों का अभाव हो, अर्थात् जिसमें तमाम प्रकार के दुर्गुण अथवा राक्षसी वृत्तियां हों । दूसरों के प्रति संवेदना, परोपकार की वृत्ति, कर्तव्यनिष्ठा, लोभ-लालच का अभाव इत्यादि अपेक्षित गुण हैं, जो अमानुष में देखने को नहीं मिलते । इन गुणों से युक्त व्यक्ति सामान्य मनुष्य की तुलना में श्रेष्ठतर माना जाएगा ।
वर्तमान युग में ये मानवीय गुणों की बातें कही तो जाती हैं, परंतु कम ही लोग होते हैं जो अपने आचरण में इन्हें अपनाने का संकल्प लेते हैं ।
आक्रुष्यमानो नाक्रोशेन्मन्युरेव तितिक्षतः।
आक्रोष्टारं निर्दहति सुकृतं चास्य विन्दति ॥
(पूर्वोक्त, श्लोक 7)
(आक्रुष्यमानः न आक्रोशेत् मन्युः एव तितिक्षतः, आक्रोष्टारं निर्दहति अस्य सुकृतं च विन्दति ।)
अर्थ – यदि अपशब्दों के द्वारा आक्रोशित किया जा रहा हो तो तज्जन्य आक्रोष अथवा क्रोध को सह लेना चाहिए । ऐसा करना आक्रोश पैदा करने वाले को ही जला डालता है और उसके सत्कर्म का फल सहने वाले को प्राप्त होता हो जाता है ।
आक्रोश तथा क्रोध में अंतर होता है । पहले में व्यक्ति अपनी नाराजगी चीखकर, डांट-डपटकर, अपशब्द बोलकर या गाली-गलौज की भाषा से व्यक्त करता है । ऐसा करने से वह ‘मैंने खरी-खोटी सुना दी’ के अहंभाव से संतुष्ट हो जाता है । तत्पश्चात् बात अक्सर आई-गई हो जाती है । किंतु क्रोध की अवस्था में व्यक्ति मारपीट करने और भौतिक रूप से हानि पहुंचाने तक को उतारू हो जाता है । उसका गुस्सा अधिक स्थाई होता है और कभी-कभी हानि पहुंचाने की योजना तक बन जाती है । पहले पक्ष की अनुचित हरकतें जब दूसरा पक्ष शांति से सह लेता है तो कदाचित् पहले पक्ष के मन में हारमान हो जाने का भाव पैदा हो जाता है । अहंकारवश वह अपनी गलती मानने को तैयार तो नहीं हो पाता, किंतु मन ही मन असफल हो जाने का दंश झेलता है । ‘निर्दहति’ या ‘जला डालता है’ कहने का मतलब यही होगा ऐसा मेरा सोचना है । लेकिन उसके सत्कर्म का फल क्रोध सहने वाले को कैसे मिलता है यह मैं नहीं कह सकता ।
दूसरे के अप्रिय व्यवहार को सहज भाव से सह लेना स्वयं में शांति प्रदान करता है यही पर्याप्त है । असहिष्णु व्यक्ति का मन बदले की आग से अशांत तो हो ही जाता है । – योगेन्द्र जोशी
24 जनवरी 2013
by योगेन्द्र जोशी
in नीति, महाभारत, वन-संरक्षण, संस्कृत-साहित्य, सूक्ति, Mahabharata, Morals, Sanskrit Literature
टैग्स: तालाब तथा जलाशय, परलोक, महाभारत, वृक्ष की उपयोगिता, वृक्षरोपण की महत्ता, importance of tree plantation, Mahabharat, ponds and water pools, the other world, usefulness of tree
विगत ५ तारीख (जनवरी) और उसके पहले की चिट्ठा-प्रविष्टियों में महाभारत महाकाव्य के एक प्रकरण (भीष्म पितामह द्वारा महाराज युधिष्ठिर को दिये गये वृक्षों एवं जलाशयों की महत्ता के उपदेश) का जिक्र किया गया था । उसी से संबंधित इस अंतिम किश्त में नीति विषयक अन्य दो श्लोकों का उल्लेख मैं आगे कर रहा हूं:
तडागकृत् वृक्षरोपी इष्टयज्ञश्च यो द्विजः ।
एते स्वर्गे महीयन्ते ये चान्ये सत्यवादिनः ॥
(महाभारत, अनुशासन पर्व, अध्याय 58, श्लोक 32)
(तडाग-कृत् वृक्ष-रोपी इष्ट-यज्ञः च यः द्विजः, एते स्वर्गे महीयन्ते ये च अन्ये सत्य-वादिनः ।)
अर्थ – तालाब बनवाने, वृक्षरोपण करने, अैर यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले द्विज को स्वर्ग में महत्ता दी जाती है; इसके अतिरिक्त सत्य बोलने वालों को भी महत्व मिलता है ।
द्विज का शाब्दिक अर्थ है जिसका दूसरा जन्म हुआ हो । हिंदु परंपरा के अनुसार आम तौर पर तीन वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, एवं वैश्य के लिए द्विज शब्द प्रयुक्त होता है जिनमें यज्ञोपवीत की प्रथा रही है । यह बात कर्मकांडों से जुड़ी है । गहराई से सोचा जाए तो द्विज का अर्थ संस्कारित व्यक्ति से है । कहा गया है “जन्मना जायते शूद्र संस्कारैर्द्विज उच्यते” । अर्थात् जन्म से तो सभी शूद्र ही पैदा होते हैं, संस्कारित होने से ही वह द्विज होता है । संस्कारवान् से तात्पर्य है सदाचरण का जिसे पाठ दिया जा चुका हो, जैसा यज्ञोपवीत के समय किया जाता है । मात्र जनेऊ धारण करने से संस्कारित नहीं हो जाता है कोई; असल बात सदाचरण से बनती है । मैं समझता हूं उक्त श्लोक में द्विज का निहितार्थ यही है ।
यज्ञ का अर्थ सामान्यतः समिधा से प्रज्वलित अग्निकुंड में घी-तिल-जौ जैसे हवनीय सामग्री से हवन करने से लिया जाता हैं । किंतु मैं मानता हूं कि यज्ञ के अर्थ इससे अधिक व्यापक हैं । मेरी राय में यज्ञ का अर्थ विविध कर्तव्यों के संपादन से लिया जाना चाहिए जिनकी मनुष्य से अपेक्षा की जाती है । कदाचित् इसीलिए शास्त्रों में पंच महायज्ञों (भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, एवं ब्रह्मयज्ञ) का उल्लेख मिलता है, जो मनुष्य और मनुष्येतर प्राणियों, पितरों, आदि के प्रति समर्पित रहते हैं । (देखें https://vichaarsankalan.wordpress.com/2010/09/07/ऋग्वैदिक-सूक्ति-आनोभद्र/)सत्य बोलने की महत्ता को तो विश्व के सभी समाजों में मान्यता प्राप्त है, भले ही व्यवहार में तदनुरूप आचरण विरले ही करते हों ।
तस्मात्तडागं कुर्वीत आरामांश्चैव रोपयेत् ।
यजेच्च विविधैर्यज्ञैः सत्यं च सततं वदेत् ॥
(पूर्वोक्त, श्लोक 33)
(तस्मात् तडागं कुर्वीत आरामान् च एव रोपयेत्, यजेत् च विविधैः यज्ञैः सत्यं च सततं वदेत् ।)
अर्थ – उपर्युक्त बातों को दृष्टि में रखते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह तालाबों का निर्माण करे/करवाए; बाग-बगीचे बनवाए; विविध प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करे; और सत्य बोलने का संकल्प ले ।
आराम शब्द संस्कृत के रम् क्रियाधातु से बना है, जिसका अर्थ है आनंद अनुभव करना, प्रसन्न होना, रम जाना आदि । उसके अनुसार आराम का अर्थ बाग-बगीचा, पार्क, रमणीय स्थल, घूमने-फिरने का स्थान आदि लिया जा सकता है । मनुष्य को ऐसे स्थलों का निर्माण कराना चाहिए । यज्ञ का व्यापक अर्थ मैंने हितकर कर्तव्यों के संपादन से लिया है । मनुष्य सत्कर्म करे और मिथ्या भाषण न करे यही संदेश इस श्लोक से लिया जा सकता है । – योगेन्द्र जोशी
05 जनवरी 2013
by योगेन्द्र जोशी
in नीति, महाभारत, लोकव्यवहार, वन-संरक्षण, संस्कृत-साहित्य, Mahabharata, Morals, Sanskrit Literature
टैग्स: परलोक, महाभारत, वृक्ष की उपयोगिता, वृक्षरोपण की महत्ता, importance of tree plantation, Mahabharat, the other world, usefulness of tree
मैंने १६ अक्टूबर एवं १२ नवंबर के आलेखों में महाभारत महाकाव्य के एक प्रकरण का जिक्र किया था, जिसमें भीष्म पितामह द्वारा महाराज युधिष्ठिर को दिये गये वृक्षों एवं जलाशयों की महत्ता के उपदेश का वर्णन किया गया है । कई हफ़्तों के बाद मैं उसी विषय पर अगले दो श्लोकों को यहां उद्धृत कर रहा हूं:
पुष्पिताः फलवन्तश्च तर्पयन्तीह मानवान् ।
वृक्षदं पुत्रवत् वृक्षास्तारयन्ति परत्र च ॥
(महाभारत, अनुशासन पर्व, अध्याय 58, श्लोक 30)
(इह पुष्पिताः फलवन्तः च मानवान् तर्पयन्ति, वृक्षाः वृक्षदं पुत्रवत् परत्र च तारयन्ति ।)
अर्थ – फलों और फूलों वाले वृक्ष मनुष्यों को तृप्त करते हैं । वृक्ष देने वाले अर्थात् समाजहित में वृक्षरोपण करने वाले व्यक्ति का परलोक में तारण भी वृक्ष करते हैं ।
पेड़-पौधों का महत्व फल-फूलों के कारण होता ही हैं । अन्य प्रकार की उपयोगिताएं भी उनसे जुड़ी हैं, जैसे पथिकों को छाया, गृहस्थों को जलाने के लिए इंधन, भवन निर्माण के लिए लकड़ी, इत्यादि । स्वर्ग-नर्क में विश्वास करने वालों के मतानुसार परलोक में मनुष्य का तारण पुत्र करता है । इस नीति वचन के अनुसार वृक्ष भी पुत्रवत् उसका तारण करते हैं ।
तस्मात् तडागे सद्वृक्षा रोप्याः श्रेयोऽर्थिना सदा ।
पुत्रवत् परिपाल्याश्च पुत्रास्ते धर्मतः स्मृताः ॥
(पूर्वोक्त, श्लोक 31)
(तस्मात् श्रेयस्-अर्थिना तडागे सद्-वृक्षा सदा रोप्याः पुत्रवत् परिपाल्याः च, ते धर्मतः पुत्राः स्मृताः ।)
अर्थ – इसलिए श्रेयस् यानी कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह तालाब के पास अच्छे-अच्छे पेड़ लगाए और उनका पुत्र की भांति पालन करे । वास्तव में धर्मानुसार वृक्षों को पुत्र ही माना गया है ।
वृक्षों की उपयोगिता देखते हुए उनको पुत्र कहा गया है । जिस प्रकार मनुष्य अपने पुत्र का लालन-पालन करता है वैसे ही वृक्षों का भी करे । जैसे सुयोग्य पुत्र माता-पिता एवं समाज का हित साधता है वैसे ही वृक्ष भी समाज के लिए हितकर होते हैं ।
मेरा मानना है कि नीतिवचनों में जहां कहीं पुत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां उसका अर्थ संतान समझना चाहिए । इस संसार में पुत्र एवं पुत्री की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण समझी जानी चाहिए, क्योंकि प्राणीजगत् में दोनो की महत्ता समान रूप से देखी जाती है । – योगेन्द्र जोशी
12 नवम्बर 2012
by योगेन्द्र जोशी
in नीति, महाभारत, वन-संरक्षण, संस्कृत-साहित्य, Mahabharata, Morals, Sanskrit Literature
इस चिठ्ठे की पिछली प्रविष्टि (16 अक्टूबर) में मैंने इस बात की चर्चा की थी कि महाभारत महाकाव्य के एक प्रकरण में भीष्म पितामह द्वारा महाराज युधिष्ठिर को वृक्षों एवं जलाशयों की महत्ता के उपदेश का वर्णन किया गया है । उसी विषय पर उपलब्ध अगले दो श्लोकों को यहां उद्धृत किया जा रहा है:
पुष्पैः सुरगणान् वृक्षाः फलैश्चापि तथा पितॄन् ।
छायया चातिथिं तात पूजयन्ति महीरुहः ॥
(महाभारत, अनुशासन पर्व, अध्याय 58, श्लोक 28)
(पुष्पैः सुर-गणान् वृक्षाः फलैः च अपि तथा पितॄन्, छायया च अतिथिं तात पूजयन्ति महीरुहः ।)
अर्थ – हे मेरे तात युधिष्ठिर, वृक्षवृंद अपने फूलों से देवताओं को और उसी प्रकार फलों से पितरों की पूजा करते हैं । इसके अलावा ये वृक्ष अपनी छाया द्वारा अतिथि जनों के प्रति सम्मान दर्शाते हैं ।
तात्पर्य यह है कि पेड़ों से प्राप्त फल-फूलों के माध्यम से ही देवों-पितरों की पूजा-अर्चना की जाती है । थके-मांदे अतिथि (पथिक) को इनसे विश्राम हेतु छाया प्राप्त होती है । इसलिए इनकी महत्ता सर्वस्वीकार्य है ।
किन्नरोरगरक्षांसि देवगन्दर्भमानवाः ।
तथा ऋषिगणाश्चैव संश्रयन्ति महीरुहान् ॥
(पूर्वोक्त, श्लोक 29)
(किन्नर-उरग-रक्षांसि देव-गन्दर्भ-मानवाः, तथा ऋषि-गणाः च एव महीरुहान् संश्रयन्ति ।)
अर्थ – किन्नर, उरग, राक्षस, देवता, मनुष्य और ऋषियों के समूह वृक्षों का आश्रय स्वीकारते है ।
मैं इस श्लोक का अर्थ ठीक से नहीं समझ सका हूं । यहां उल्लिखित किन्नर आदि के वास्तव में क्या तात्पर्य हैं ? उरग शब्द सामान्यतः सरीसृप प्रजाति के जीवधारियों के लिए प्रयुक्त होता है । यों किन्नर का शाब्दिक अर्थ है विकृत पुरुष – पुरुष जिसमें मानसिक अथवा शारीरिक तौर पर विकार हो । आजकल यौनांगों की विकृति वालों को किन्नर पुकारा जाता है । पौराणिक कथाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि किन्नर मानवशरीरधारी जीव थे । मैं मानता हूं कि वे मानवों की एक जाति थी जो स्वयं को सभ्य कहने वाले आर्यों के क्षेत्र से दूर अलग प्रकार की जीवन शैली वाले लोग थे । कुछ ऐसी ही बात राक्षसों के लिए लागू होती है, जो मानवशरीरधारी उग्र स्वभाव वाले, उत्पाती, एवं आर्यों की नजर में ‘असभ्य’ रहे होंगे । देवताओं को उच्च क्षमताओं के पूज्य ‘प्राणी’ समझा जाता था । नृत्य गायन आदि में पारंगत जाति गंदर्भ कही जाती थी । मेरा मानना है कि ये सब वस्तुतः मनुष्यों की अलग-अलग जातियां रही होंगी । ऐसा इसलिए कि पुराणों में जैविक दृष्टि से सभी समान थे । उनके परस्पर दैहिक संसर्ग, वैवाहिक संबंधों की कथाएं पढ़ने को मिलती हैं । उरग भी एक जाति रही होगी । अगर उरग सामान्य अजगर-सांप आदि को इंगित करता होता, तो पशु शब्द का प्रयोग अधिक सार्थक होता । किन्नर, गंदर्भ आदि के साथ पशु अर्थ में उरग शामिल करना अटपटा लगता है । यों भी पुराणों में नागकन्याओं के साथ विवाह आदि की कथाएं प्रचलित हैं । इस प्रकार ये सभी शब्द मानवों की विविध जातियों को व्यक्त करते होंगे ऐसा मेरा सोचना है । श्लोक के अनुसार ये सभी पेड़.-पौधों पर अलग-अलग प्रकार से निर्भर करते हैं । – योगेन्द्र जोशी
Previous Older Entries Next Newer Entries